प्रेम, परम्परा और विद्रोह
कात्यायनी
![Prem, Parampara aur vidroh Final]() बाबू बजरंगी आज एक राष्ट्रीय परिघटना बन चुका है। अहमदाबाद के इस शख़्स का दावा है कि अबतक वह सैकड़ों हिन्दू कन्याओं को "मुक्त"करा चुका है। "मुक्ति"का यह काम बाबू बजरंगी मुस्लिम युवकों के साथ हिन्दू युवतियों के प्रेमविवाह को बलपूर्वक तुड़वाकर किया करता है। ज़ाहिर है कि अन्तर्धार्मिक विवाहों, या यूँ कहें कि दो व्यस्कों द्वारा परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध कायम करने के स्वतंत्र निर्णय को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद बाबू बजरंगी का "मुक्ति अभियान"यदि अबतक निर्बाध चलता रहा है तो इसके पीछे गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा प्राप्त परोक्ष सत्ता-संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण हाथ है।
बाबू बजरंगी आज एक राष्ट्रीय परिघटना बन चुका है। अहमदाबाद के इस शख़्स का दावा है कि अबतक वह सैकड़ों हिन्दू कन्याओं को "मुक्त"करा चुका है। "मुक्ति"का यह काम बाबू बजरंगी मुस्लिम युवकों के साथ हिन्दू युवतियों के प्रेमविवाह को बलपूर्वक तुड़वाकर किया करता है। ज़ाहिर है कि अन्तर्धार्मिक विवाहों, या यूँ कहें कि दो व्यस्कों द्वारा परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध कायम करने के स्वतंत्र निर्णय को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद बाबू बजरंगी का "मुक्ति अभियान"यदि अबतक निर्बाध चलता रहा है तो इसके पीछे गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा प्राप्त परोक्ष सत्ता-संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण हाथ है।
लेकिन बात सिर्फ़ इतनी ही नहीं है। नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा, जो साम्प्रदायिक कट्टरपंथी नहीं है, वह भी अपने रूढ़िवादी मानस के कारण, अन्तर्जातीय-अन्तर्धार्मिक प्रेम विवाहों का ही विरोधी है और बाबू बजरंगी जैसों की हरकतों के निर्बाध जारी रहने में समाज के इस हिस्से की भी एक परोक्ष भूमिका होती है। समाज के पढ़े-लिखे, प्रबुद्ध माने जाने वाले लोगों का बहुलांश आज भी ऐसा ही है जो युवाओं के बीच प्रेम सम्बन्ध को ही ग़लत मानता है और उसे अनाचार अनैतिकता की कोटि में रखकर देखता है। बहुत कम ही ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बेटों या बेटियों के प्रेम सम्बन्ध को सहर्ष स्वीकार करते हों और अपनी ज़िन्दगी के बारे में निर्णय लेने के उनके अधिकार को दिल से मान्यता देते हों। यदि वे स्वीकार करते भी हैं तो ज्यादातर मामलों में विवशता और अनिच्छा के साथ ही। और जब बात किसी अन्य धर्म के या अपने से निम्न मानी जाने वाली किसी जाति (विशेषकर दलित) के युवक या युवती के साथ, अपने बेटे या बेटी के प्रेम की हो तो अधिकांश उदारमना माने जाने वाले नागरिक भी जो रुख अपनाते हैं, उससे यह साफ़ हो जाता है कि हमारे देश का उदार और सेक्युलर दिलो-दिमाग़ भी वास्तव में कितना उदार और सेक्युलर है! यही कारण है कि जब धर्म या जाति से बाहर प्रेम करने के कारण किसी बेटी को अपने ही घर में काटकर या जलाकर मार दिया जाता है या किसी दलित या मुस्लिम युवक को सरेआम फ़ाँसी पर लटकाकर मार दिया जाता है या उसकी बोटी–बोटी काट दी जाती है या उसके परिवार को गाँव-शहर छोड़ने तक पर मज़बूर कर दिया जाता है तो ऐसे मसलों को लेकर केवल महानगरों का सेक्युलर और प्रगतिशील बुद्धिजीवी समुदाय ही (गौरतलब है कि ऐसे बुद्धिजीवी महानगरीय बुद्धिजीवियों के बीच भी अल्पसंख्यक ही हैं) कुछ चीख-पुकार मचाता है, शासन–प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की माँग की जाती है, कुछ प्रतीकात्मक धरने-प्रदर्शन होते हैं, कुछ जाँच टीमें घटनास्थल का दौरा करती हैं, अखबारों में लेख-टिप्पणियाँ छपती हैं (और लगे हाथों फ्रीलांसर नामधारियों की कुछ कमाई भी हो जाती है), टी.वी. चैनलों को 'मुकाबला', 'टक्कर'या ऐसे ही नाम वाले किसी कार्यक्रम के लिए मसाला मिल जाता है और कुछ प्रचार–पिपासु, धनपिपासु सेक्युलर बुद्धिजीवियों को भी अपनी गोट लाल करने का मौका मिल जाता है। जल्दी ही मामला ठण्डा पड़ जाता है और फ़िर ऐसे ही किसी नये मामले का इन्तज़ार होता है जो लम्बा कत्तई नहीं होता।
मुद्दा केवल किसी एक बाबू बजरंगी का नहीं है। देश के बहुतेरे छोटे-बड़े शहरों और ग्रामीण अंचलों में ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो धर्म और संस्कृति के नाम पर ऐसे कारनामों को अंजाम दिया करते हैं और बात केवल धार्मिक कट्टरपंथी फ़ासीवादी राजनीति से प्रेरित गिरोहों की ही नहीं है। ऐसे पिताओं और परिवारों के बारे में भी आये दिन खबरें छपती रहती हैं जो जाति-धर्म के बाहर प्रेम या विवाह करने के चलते अपनी ही सन्तानों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जाति-बिरादरी की पंचायतों की मध्ययुगीन सत्ता इतनी मज़बूत है कि जाति-धर्म के बाहर शादी करना तो दूर, सगोत्रीय विवाह की वर्जना तक को तोड़ने के चलते पंचायतों द्वारा सरेआम मौत की सज़ा दे दी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ़्फ़रनगर, सहारनपुर, मेरठ आदि जिलों से लेकर हरियाणा तक से हर वर्ष ऐसी कई घटनाओं की खबरें आती रहती हैं और उससे कई गुना घटनाएँ ऐसी होती हैं जो खबर बन पाने से पहले ही दबा दी जाती हैं। इन सभी मामलों में पुलिस और प्रशासन का रवैया भी पूरी तरह पंचायतों के साथ हुआ करता है। अपने जातिगत और धार्मिक पूर्वाग्रहों के चलते पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों की सहानुभूति भी पंचायतों के रूढ़िवादी बड़े-बुजुर्गों के साथ ही हुआ करती है। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी इन पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होती। आये दिन दिल्ली-मुम्बई से लेकर देश के छोटे-छोटे शहरों तक में पार्कों-सिनेमाघरों-कैम्पसों आदि सार्वजनिक स्थानों पर घुसकर बजरंगियों-शिवसैनिकों और पुलिस द्वारा प्रेमी जोड़ों की पिटाई को भी इसी आम सामाजिक प्रवृत्ति से जोड़कर देखा जाना चाहिए क्योंकि आम लोग ऐसी घटनाओं का मुखर प्रतिवाद नहीं करते।
कहा जा सकता है कि प्रेम करने की आज़ादी सहित किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत आज़ादी, निजता और निर्णय की स्वतंत्रता के विरुद्ध एक बर्बर किस्म की निरंकुशता पूरी भारतीय सामाजिक संरचना के ताने-बाने में सर्वव्याप्त प्रतीत होती है। सोचने की बात यह है कि उत्पादन की आधुनिक प्रक्रिया अपनाने, आधुनिकतम, उपभोक्ता सामग्रियों का इस्तेमाल करने और भौतिक जीवन में आधुनिक तौर–तरीके अपनाने के बावजूद हमारे समाज में निजता, व्यक्तिगत आज़ादी, तर्कणा आदि आधुनिक जीवन–मूल्यों का सामाजिक-सांस्कृतिक वर्चस्व आजतक क्यों नहीं स्थापित हो सका? भारत में सतत् विकासमान पूँजीवाद मध्ययुगीन मूल्यों-मान्यताओं के साथ इतना कुशल-सफ़ल तालमेल क्यों और किस प्रकार बनाये हुए है? इस बात को सुसंगत ढंग से केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है।
यह सही है कि आज का पश्चिमी समाज समृद्धि के शिखर पर आसीन होने के बावजूद, आर्थिक स्तर पर असाध्य ढाँचागत संकट, राजनीतिक स्तर पर पूँजीवादी जनवाद के क्षरण एवं विघटन तथा सांस्कृतिक-सामाजिक स्तर पर विघटन, अलगाव, नैतिक अधःपतन और अराजकता का शिकार है। पारिवारिक ढाँचे का ताना-बाना वहाँ बिखर रहा है। अपराधों, मानसिक रोगों और आत्मिक वंचना का ग्राफ़ लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया को लूटकर समृद्धि का द्वीप बसाने वाले पश्चिमी महाप्रभुओं से इतिहास उनकी करनी का वाजिब हिसाब वसूल रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम में नागरिकों के आपसी रिश्तों और परिवार सहित सभी सामाजिक संस्थाओं में जनवाद के मूल्य इस तरह रचे-बसे हुए हैं कि कैथोलिक, प्रोटेस्टैण्ट, यहूदी, मुसलमान, श्वेत, अश्वेत-किसी भी धर्म या नस्ल के व्यक्ति यदि आपस में प्यार या शादी करें तो सामाजिक बॉयकॉट या पंचायती दण्ड जैसी किसी बात की तो कल्पना तक नहीं की जा सकती। हो सकता है कि परिवार की पुरानी पीढ़ी कहीं-कहीं इस बात का विरोध करे, पर यह विरोध प्रायः उसूली मतभेद के दायरे तक ही सीमित रहता है। जहाँ तक समाज का सम्बन्ध है, लोग इसे किन्हीं दो व्यक्तियों का निजी मामला ही मानते हैं। यह सही है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों में अश्वेतों और अन्य अप्रवासियों का पार्थक्य, दोयम दर्जे की आर्थिक स्थिति और उनके प्रति विद्वेष भाव लगातार मौजूद रहता है और पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ नवनात्सीवादी गिरोह इन्हें हिंसा और गुण्डागर्दी का भी शिकार बनाते रहे हैं। धनी-गरीब के अन्तर और वर्ग-अन्तरविरोध भी वहाँ तीखे रूप में मौजूद हैं। लेकिन सामाजिक ताने-बाने में वहाँ निजता और व्यक्तिगत आज़ादी के जनवादी मूल्य इस तरह रचे-बसे हैं कि धर्म या नस्ल के बाहर प्रेम या विवाह को मन ही मन गलत मानने वाले लोग भी इसका संगठित और मुखर विरोध नहीं करते। पश्चिम में 'मैचमेकर्स'द्वारा परिवारों के बीच बातचीत करके शादियाँ कराने की परम्परा उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक ही दम तोड़ने लगी थी। प्रेम और विवाह के मामलों में वहाँ के समाज में मुख्य और स्थापित प्रवृत्ति युवाओं को पूरी आज़ादी देने की है। इसका मुख्य कारण है कि मानववाद, इहलौकिकता, वैयक्तिकता और जनवाद के मूल्यों को सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलनों और क्रान्तियों के कई शताब्दियों लम्बे सिलसिले ने यूरोपीय समाज के पोर–पोर में इस कदर रचा-बसा दिया था कि साम्राज्यवाद की एक पूरी सदी बीत जाने के बावजूद, पश्चिमी पूँजीवाद राज्यसत्ताओं के बढ़ते निरंकुश चरित्र और पूँजीवादी जनवाद के पतन–विघटन की प्रक्रिया के समापन बिन्दु के निकट पहुँचने के बावजूद, तमाम सामाजिक विषमताओं, आर्थिक लूट, सामाजिक-सांस्कृतिक-नैतिक अधःपतन तथा पण्यपूजा (कमोडिटी फ़ेटिशिज्म) और अलगाव (एलियनेशन) के घटाटोप के बावजूद वहाँ नागरिकों के आपसी रिश्तों और मूल्यों-मान्यताओं में व्यक्तियों की निजता और व्यक्तिगत आज़ादी को पूरा सम्मान देने की प्रवृत्ति आज भी अनुत्क्रमणीय रूप से स्थापित है। पंचायती न्याय की मध्ययुगीन कबीलाई बर्बरता के बारे में, अन्तर्धार्मिक अन्तर्जातीय विवाह करने पर सामाजिक बहिष्कार, अपना गाँव-शहर छोड़ने के लिए विवश होने या हत्या तक की कीमत चुकाने के बारे में या प्रेमी जोड़ों की पार्कों में सामूहिक पिटाई जैसी घटना के बारे में वहाँ का एक आम नागरिक सोच तक नहीं सकता।
यूरोपीय पूँजीवादी समाज पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति (रिनेसां-एनलाइटेनमेण्ट-रिवोल्यूशन) की शताब्दियों लम्बी प्रक्रिया से गुजरकर अस्तित्व में आया था। इस प्रक्रिया में अधिकांश मध्ययुगीन मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं का वर्चस्व वहाँ लगभग समाप्त हो गया था। यद्यपि सत्तासीन होने के बाद यूरोपीय पूँजीपति वर्ग ने चर्च से "पवित्र गठबन्धन"करके तर्कणा और जनवाद के झण्डे को धूल में फ़ेंक दिया और पुनर्जागरण-प्रबोधन के समस्त मानववादी-जनवादी आदर्शों को तिलांजलि दे दी, लेकिन ये मूल्य सामाजिक-सांस्कृतिक अधिरचना के ताने-बाने में इस कदर रच-बस चुके थे कि सामाजिक जनमानस में इनकी अन्तर्व्याप्ति को समूल नष्ट करके मध्ययुग की ओर वापस नहीं लौटा जा सकता था। पूँजीवाद के ऐतिहासिक विश्वासघात और असली चरित्र को उजागर करने में उन्नीसवीं शताब्दी के आलोचनात्मक यथार्थवादी कला-साहित्य ने भी एक विशेष भूमिका निभायी। यह तुलनात्मक अध्ययन अलग से पर्याप्त गहराई और विस्तार की माँग करता है, जो यहाँ सम्भव नहीं है।
भारतीय इतिहास की गति और दिशा इस सन्दर्भ में यूरोप से सर्वथा भिन्न रही है। यहाँ मध्ययुगीन सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक संरचना का ताना-बाना जब अन्दर से टूटने-बिखरने की दिशा में अग्रसर था और इसके भीतर से प्रगतिशील पूँजीवादी तत्वों के उद्भव और विकास की प्रक्रिया गति पकड़ रही थी, उसी समय देश के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी। उपनिवेशीकरण की व्यवस्थित प्रक्रिया ने एक शताब्दी के भीतर भारतीय समाज की स्वाभाविक आन्तरिक गति की हत्या कर दी और यहाँ की संक्रमणशील देशज सामाजिक-आर्थिक संरचना को नष्ट करके ऊपर से एक औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना आरोपित कर दी। निश्चय ही भारतीय मध्ययुगीन सामाजिक-आर्थिक संरचना की अपनी विशिष्टताएँ थीं, यह यूरोपीय सामन्तवाद से काफ़ी भिन्न थी और यहाँ पूँजीवादी विकास बहुतेरी बाधाएँ-समस्याएँ भी थीं। लेकिन ये बाधाएँ पूँजीवादी विकास को रोक नहीं सकती थीं। प्राक्-ब्रिटिश भारत में पूँजीवादी विकास के उपादान मौजूद थे। यदि भारत उपनिवेश नहीं बनता तो उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ ही पूँजी भारतीय समाज के पोर–पोर में घुस जाती और फ़िर वह समय भी आता जब एक सर्वसमावेशी सामाजिक झंझावात के साथ यहाँ भी इतिहास को तेज़ गति देने वाला पूँजीवाद अपनी भौतिक-आत्मिक समग्रता के साथ अस्तित्व में आता। मध्ययुगीन समाज के परमाणु नाभिक पर सतत् प्रहार उसे विखण्डित कर देते और ऊर्जा का अजय स्रोत फ़ूट पड़ता। मुख्यतः किसानों-दस्तकारों की शक्ति से संगठित मध्यकालीन भारत के भक्ति आन्दोलन और किसान संघर्षों ने इस दिशा में एक पूर्वसंकेत दे भी दिया था। तमाम पारिस्थितिक भिन्नताओं के बावजूद भारतीय भक्ति आन्दोलन और यूरोपीय धर्म-सुधार आन्दोलन में तात्विक समानता के बहुतेरे अवयव मौजूद दीखते हैं। भारतीय इतिहास हूबहू पुनर्जागरण-प्रबोधन-बुर्जुआ क्रान्ति के यूरोपीय मार्ग का अनुकरण करता हुआ आगे बढ़ता, यह मानना मूर्खता होगी। रूस और जापान जैसे देशों ने भी पूँजीवादी विकास का अपना सापेक्षतः भिन्न मार्ग चुना था और यूरोप में भी जर्मनी और पूर्वी यूरोपीय देशों का रास्ता ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों से काफ़ी भिन्नता लिये हुए था। लेकिन इतना तय है कि यदि भारत का उपनिवेशीकरण नहीं होता तो अपनी स्वाभाविक गति और प्रक्रिया से यहाँ जो पूँजीवाद विकसित होता, वह आज के भारतीय पूँजीवाद जैसा रुग्ण-बौना-विकलांग नहीं होता। उसमें इतनी शक्ति होती कि वह मध्ययुगीन आर्थिक मूलाधार के साथ ही अधिरचना को भी चकनाचूर कर देता। यहाँ भी यूरोपीय पुनर्जागरण-प्रबोधन की भाँति कुछ आमूलगामी सामाजिक-सांस्कृतिक-वैचारिक तफ़ूान उठ खड़े होते जो मानववाद, जनवाद और तर्कणा के मूल्यों को समाज के रूंध्र-रूंध्र में पैठा देते। ऐसी स्थिति में भारतीय मानस भी प्राचीन भारत की भौतिकवादी चिन्तन-परम्परा का पुनःस्मरण करता और दर्शन–कला-साहित्य से लेकर जीवन–मूल्यों तक के धरातल में जुझारू भौतिकवादी चिन्तन की एक सशक्त आधुनिक परम्परा अस्तित्व में आती। लेकिन उपनिवेशीकरण ने इन सभी सम्भावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने न केवल पूरे देश को समुद्री डाकुओं से भी अधिक बर्बर तरीके से लूटा-खसोटा, बल्कि उनकी नीतियों ने यहाँ कृषि से दस्तकारी और दस्तकारी से उद्योग तक की स्वाभाविक यात्रा की सारी सम्भावनाओं की भ्रूण हत्या कर दी। भूमि के औपनिवेशिक बन्दोबस्त ने भारत में एक नये किस्म की अर्द्धर्सामन्ती भूमि-व्यवस्था को जन्म दिया। विश्व प्रसिद्ध भारतीय दस्तकारी तबाह हो गयी और भारत की आर्थिक-सामाजिक गतिकी अपनी स्वतंत्र गति और स्वतंत्र सम्भावनाओं के साथ अकाल मृत्यु का शिकार हो गयी। इसकी दिशा और नियति पूरी तरह से ब्रिटिश वित्तीय पूँजी के हितों के अधीन हो गयी।
जिसे भारतीय इतिहासकार प्रायः "भारतीय पुनर्जागरण"की संज्ञा से विभूषित करते हैं, उसमें यूरोपीय पुनर्जागरण जैसा क्रान्तिकारी कुछ भी नहीं था। वह कोई महान या प्रगतिशील जनक्रान्ति कतई नहीं थी। वह औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना के भीतर पले-बढ़े एक छोटे से पढ़े-लिखे मध्यवर्ग की आवाज़ थी जो स्वामिभक्त ब्रिटिश प्रजा के रूप में कुछ अधिकारों की याचना कर रहा था। भारतीय समाज में सुधारों की इसकी माँग और इसके सुधार आन्दोलनों का प्रभाव शहरी मध्यवर्ग तक सीमित था और किसान–दस्तकार तथा आम मेहनतकश जनता उससे सर्वथा अछूती थी। आज़ादी की आधी सदी बाद भी भारतीय बौद्धिक जगत की निर्वीर्यता, जनविमुखता और कायरता इसी बात का प्रमाण है कि भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण या प्रबोधन जैसी कोई चीज़ कभी घटित ही नहीं हुई। हमारी सामाजिक संरचना में जनवाद और तर्कणा के मूल्यों के अभाव और आधुनिक पूँजीवादी जीवन–प्रणाली के साथ मध्ययुगीन मूल्यों-मान्यताओं का विचित्र सहअस्तित्व भी दरअसल इसी तथ्य को प्रमाणित करता है।
औपनिवेशिक काल में भारत में जिस पूँजीवाद का विकास हुआ, वह किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन का नहीं, बल्कि ब्रिटिश वित्तीय पूँजी के हितसाधन के लिए उठाये गये कदमों की गौण गति का परिणाम था जो उपनिवेशवादियों की इच्छा से स्वतंत्र था। इस मरियल, रीढ़विहीन पूँजीवाद की स्वाभाविक गति को भी उपनिवेशवाद ने कदम-कदम पर नियंत्रित और बाधित करने का काम किया। लेकिन इतिहास की गति शासक वर्गों के इच्छानुकूल नहीं होती और उनके द्वारा उठाया गया हर कदम स्वयंस्फ़ूर्त ढंग से एक प्रतिरोधी गति एवं प्रभाव को गौण पहलू के रूप में जन्म देता है और फ़िर कालान्तर में यह गौण पहलू मुख्य पहलू भी बन जाया करता है। औपनिवेशिक काल में भारत में पूँजीवाद का विकास इसी रूप में हुआ और फ़िर उपनिवेशवाद के संकट, अन्तरसाम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और विश्वयुद्धों का लाभ उठाकर भारतीय पूँजीपति वर्ग ने अपनी शक्ति बढ़ाने का काम किया। अपनी बढ़ती शक्ति के अनुपात में ही इसकी आवाज़ भी मुखर होती गयी और फ़िर एक दिन इसने राजनीतिक आज़ादी भी हासिल कर ली, लेकिन यह राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति जैसा कुछ भी नहीं था। भारतीय पूँजीवाद ने साम्राज्यवाद से निर्णायक विच्छेद करने के बजाय उसके कनिष्ठ सहयोगी की भूमिका निभाई और भूमि क्रान्ति के जनवादी कार्यभार को भी एक झटके के साथ पूरा करने के बजाय क्रमिक पूँजीवादी रूपान्तरण का दुस्सह यंत्रणादायी प्रतिगामी पथ अपनाया। ज़ाहिर है कि ऐसी स्थिति में सामाजिक-सांस्कृतिक-वैचारिक अधिरचना में भी, औपनिवेशिक काल और उत्तर औपनिवेशिक काल में कभी क्रान्तिकारी परिवर्तन की कोई प्रक्रिया घटित ही नहीं हुई। यूरोपीय पूँजीवाद कम से कम पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति की प्रक्रिया में जनता के साथ जुड़ा हुआ और प्रगतिशील मूल्यों का वाहक था। भारत में ऐसी कोई प्रक्रिया घटित ही नहीं हुई। भारतीय पूँजीपति वर्ग ने शुरू से ही प्राक्-पूँजीवादी मूल्यों-मान्यताओं के साथ समझौते का रुख अपनाया और साम्राज्यवाद की सदी में क्रमिक विकास की प्रक्रिया में जिन बुर्जुआ मूल्यों को इसने क्रमशः अपनाया, वे तर्कणा, मानववाद, जनवाद और जुझारू भौतिकवाद के मूल्य नहीं थे, बल्कि सड़े-गले प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ मूल्य ही थे।
भारतीय पूँजीवाद कृषि से दस्तकारी और दस्तकारी से उद्योग की स्वाभाविक प्रक्रिया से नहीं जन्मा था। यह बर्गरों की सन्तान नहीं था। यह आरोपित औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना की सन्तान था और इसका विकास उपनिवेशवाद के अनिवार्य आन्तरिक अन्तरविरोध का परिणाम था। क्रान्तिकारी संघर्ष के बजाय इसने 'समझौता-दबाव-समझौता'की रणनीति अपनाकर राजनीतिक स्वतंत्रता तक की यात्रा तय की। इसका चरित्र शुरू से ही दुहरा था। राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्यधारा का नेतृत्व करते हुए इसने जिन वायदों-नारों पर जनसमुदाय को साथ लिया, उनसे बार-बार मुकरता रहा और विश्वासघात करता रहा। ज़ाहिर है कि औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना के गर्भ से पैदा हुआ और साम्राज्यवादी विश्व-परिवेश में पला-बढ़ा पूँजीवाद ऐसा ही हो सकता था। भारतीय समाज के औपनिवेशिक अतीत की इस त्रासदी को समझना ही राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के दौरान और आज के भारत में विभिन्न वर्गों की भूमिका को, उनके संघर्षों की कमजोरियों को, मूलाधार और अधिरचना के विविध पक्षों को, भावी परिवर्तन की दिशा और समस्याओं को तथा आज के आधुनिक पूँजीवादी समाज में पण्य-पूजा और अलगाव आदि पूँजीवादी विकृतियों के साथ-साथ मध्ययुगीन बर्बर परम्पराओं-रूढ़ियों-मान्यताओं के विचित्र सहमेल को समझने की एक कुंजीभूत कड़ी है। औपनिवेशिक अतीत के जन्मचिन्ह केवल भारतीय पूँजीपति वर्ग ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों के शरीर पर भी अंकित हैं। पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति की प्रक्रिया के हाशिए पर खड़ा रूस बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक मध्ययुगीन बर्बरता के आगोश में जकड़ा हुआ था, लेकिन चूँकि औपनिवेशिक गुलामी ने उसकी स्वतंत्र आन्तरिक गति का गला नहीं घोंटा था, इसलिए उस देश में हर्ज़ेन, बेलिंस्की, चेर्निशेव्स्की, दोब्रोल्यूबोव जैसे क्रान्तिकारी जनवादी विचारकों और पुश्किन, गोगोल, लर्मन्तोव, तुर्गनेव, तोल्स्तोय, दोस्तोयेव्स्की, कोण्रोलेंको, चेखव आदि यथार्थवादी लेखकों ने अपने कृतित्व से तथा उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यवर्गीय क्रान्तिकारियों ने अपने शौर्य से न केवल एक भावी युगान्तरकारी क्रान्ति की ज़मीन तैयार की, बल्कि क्रान्तिकारी जनवादी विचारों से पूरे सामाजिक मानस को सींचने का काम किया। चीन भी निहायत पिछड़ा और साम्राज्यवादी लूट-खसोट से तबाह देश था, लेकिन भारत की तरह उसका पूर्ण उपनिवेशीकरण नहीं हो सका। इसीलिए न केवल उस देश ने सुनयात सेन, लू शुन और माओ जैसे जननायक पैदा किये, बल्कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अन्तरराष्ट्रीय नेतृत्व पर अन्धी निर्भरता और अनुकरण के बजाय अपनी क्रान्ति का मार्ग स्वयं ढूँढ़ा। चीनी क्रान्ति ने आधी सदी के भीतर ही उत्पादन सम्बन्धों के साथ-साथ चीनी जनमानस में गहराई तक पैठे मध्ययुगीन बर्बर मूल्यों, रहस्यवाद और धार्मिक रूढ़ियों को काफ़ी हद तक उखाड़ फ़ेंका था। इस तुलना के द्वारा (ध्यान रखते हुए कि हर तुलना लँगड़ी होती है) हम कहना यह चाहते हैं कि उपनिवेशीकरण की त्रासदी ने न केवल भारतीय पूँजीपति वर्ग को, बल्कि बुद्धिजीवियों और सर्वहारा वर्ग सहित हमारे समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया तथा उनके वैचारिक-सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलनों को कमज़ोर बनाने का काम किया। निश्चय ही, राष्ट्रीय आन्दोलन और वर्ग संघर्ष की ऊष्मा ने भारत में भी राधामोहन गोकुल और राहुल सांकृत्यायन जैसे उग्र परम्पराभंजक चिन्तक, भगतसिंह जैसे युवा विचारक क्रान्तिकारी और प्रेमचन्द जैसे महान जनवादी यथार्थवादी लेखक को जन्म दिया, लेकिन क्षितिज पर अनवरत प्रज्ज्वलित इन मशालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि औपनिवेशिक भारत में किसी युगान्तरकारी वैचारिक-सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन की ज़मीन ही बहुत कमज़ोर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तिलक जैसे उग्र राष्ट्रवादी तथा युगान्तर-अनुशीलन के मध्यवर्गीय क्रान्तिकारी राष्ट्रीय मुक्ति का नया वैचारिक आधार तर्कणा एवं भौतिकवादी विश्वदृष्टि आधारित मानववाद-जनवाद के आधार पर तैयार करने के बजाय खोये हुए "गौरवशाली"अतीत की पुनर्स्थापना और धार्मिक विश्वासों का सहारा लेते थे। गाँधी भारतीय परिस्थितियों में, बुर्जुआ मानववाद की प्रतिमूर्ति कहे जा सकते हैं, लेकिन जनमानस को साथ लेने के लिए उन्होंने रूढ़ियों, धार्मिक अन्धविश्वासों और पुरातनपंथी रीतियों का भरपूर सहारा लिया। इससे ("महात्मा"बनकर) जनता को साथ लेने में तो वे सफ़ल रहे लेकिन साथ ही, रूढ़ियों-परम्पराओं को पुनःसंस्कारित करके नया जीवन देने में भी उनकी भूमिका अहम हो गयी। राष्ट्रीय आन्दोलन की विभिन्न धाराओं के अधिकांश मुख्य नायकों के विचारों की तुलना यदि वाल्तेयर, दिदेरो, रूसो या टामस पेन, जफ़ैर्सन, वाशिंगटन या हर्ज़ेन, चेर्निशेव्स्की आदि के उग्र रूढ़िभंजक विचारों से करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय आन्दोलनकालीन अधिकांश भारतीय राष्ट्रीय जनवादी विचारकों ने काफ़ी हद तक "भविष्य की कविता"के बजाय "अतीत की कविता"को अपना आदर्श और प्रेरक स्रोत बनाया और फ़लतः अपने दौर में एक प्रगतिशील भूमिका निभाने के बावजूद, दूरगामी तौर पर, वस्तुगत रूप में पुनरुत्थानवादी और रूढ़िवादी यथास्थितिवाद की ज़मीन को ही मज़बूत करने का काम किया।
आज़ादी मिलने के बाद के छह दशकों के दौरान हमारे देश में सामन्ती भूमि-सम्बन्धों के टूटने और पूँजीवादी विकास की जो क्रमिक, मंथर प्रक्रिया रही है, वह आर्थिक धरातल पर तो घोर यंत्रणादायी और जनविरोधी रही ही है, मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं के धरातल पर भी यह प्रक्रिया कुछ भी ऊर्जस्वी और सकारात्मक दे पाने की क्षमता से सर्वथा रिक्त रही है। भारतीय पूँजीपति वर्ग किसी भी सामाजिक आन्दोलन में जनसमुदाय की पहलकदमी और सृजनशीलता के निर्बन्ध होने से हमेशा ही आतंकित रहा है। इसीलिए हमारे देश में पूँजीवादी विकास का रास्ता "नीचे से"नहीं बल्कि "ऊपर से"अपनाया गया, यानी जन-पहलकदमी और सामाजिक आन्दालनों के बजाय बुर्जुआ राज्यसत्ता की नीतियों पर अमल के द्वारा यहाँ पूँजीवाद का क्रमिक विकास हुआ, जिसकी सबसे तेज़ गति चार दशक बाद 1990 के दशक में देखने को मिली, जब पूरी दुनिया साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की चपेट में आ चुकी थी।
ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक तौर पर समझा जा सकता है कि बुर्जुआ जनवाद के स्वस्थ-सकारात्मक मूल्य क्यों हमारे समाज के ताने-बाने में पैठ ही नहीं पाये। किसी नागरिक को जो सीमित जनवादी और नागरिक अधिकार तथा व्यक्तिगत आज़ादी संविधान की किताब और क़ानून की धाराएँ प्रदान करती भी हैं, उन्हें न केवल पुलिस और प्रशासन का तंत्र उस तक पहुँचने नहीं देता, बल्कि मध्ययुगीन रूढ़ियों-परम्पराओं का सामाजिक-सांस्कृतिक वर्चस्व भी उन्हें निष्प्रभावी बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। रूढ़ियों का यह सामाजिक-सांस्कृतिक वर्चस्व ही वह प्रमुख उपादान है, जिसके जरिए प्रभुत्वशाली वर्ग और उसकी राज्यसत्ता आम जनता से अपने शासन के पक्ष में "स्वयंस्फ़ूर्त"सी प्रतीत होने वाली सहमति प्राप्त करती है।
कहा जा सकता है कि भारतीय बुर्जुआ समाज क्लासिकी अर्थों में, पूरी तरह से एक नागरिक समाज नहीं बन पाया है, क्योंकि न केवल प्राक्-बुर्जुआ समाज की विविध सामुदायिक अस्मिताएँ, बल्कि मूल्य-मान्यताएँ-संस्थाएँ भी आज प्रभावी और वर्चस्वकारी रूप में मौजूद हैं। लेकिन ये मूल्य-मान्यताएँ-संस्थाएँ किसी सामन्ती अभिजन समाज की नहीं, बल्कि भारतीय बुर्जुआ वर्ग या कहें कि भारतीय बुर्जुआ समाज के नये, आधुनिक अभिजन समाज की सेवा करती हैं। जो भारतीय बुर्जुआ वर्ग नये बुर्जुआ मूल्यों के सृजन में जन्म से ही असमर्थ था उसने एक क्रमिक प्रक्रिया में अर्द्धर्सामन्ती आर्थिक सम्बन्धों को तो नष्ट किया लेकिन सामन्ती मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं को किंचित संशोधन-परिष्कार के साथ अपना लिया और बुर्जुआ राज और समाज की सेवा में, या कहें कि पूँजीवाद की सेवा में सन्नद्ध कर लिया। यह कृषि और औद्योगिक उत्पादन में तो बुर्जुआ तर्कपरकता की शिक्षा देता है, लेकिन कला-साहित्य-संस्कृति और सामाजिक जीवन में अवैज्ञानिक मध्ययुगीन मूल्यों को अक्षत बने रहने देता है और न केवल बने रहने देता है, बल्कि उन्हें खाद-पानी देने का काम भी करता है।
कुछ उदाहरण लें। दहेज एक पुरानी सामन्ती संस्था है। लेकिन आज शहरों के आधुनिक मध्यवर्ग और व्यापारियों में इसका चलन सबसे ज्'यादा है। दहेज के लिए स्त्रियाँ जला दी जाती हैं और फ़िर दहेज बटोरने के लिए एक और शादी का रास्ता साफ़ हो जाता है। यानी दहेज, व्यापार या उद्यम के लिए पूँजी जुटाने का एक माध्यम बन गया है, न कि सामन्ती शान का प्रतीक रह गया है। यही कारण है कि पहले दहेज का खूब प्रदर्शन होता था, पर आज यह छिपाकर, पर्दे की ओट में ले लिया जाता है। सभी बुर्जुआ चुनावी पार्टियाँ अपनी नीतियाँ बुर्जुआ शासक वर्गों के हितसाधन के लिए तैयार करती हैं और आम लोग भी जानते होते हैं कि उनमें से कोई भी उनकी ज़िन्दगी में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन भारत में वोट बैंक की राजनीति किसी भी लोकलुभावन आर्थिक वायदे या राजनीतिक नारे से अधिक जातिगत समीकरणों पर आधारित होती है। जातियों और उनकी पंचायतों के मुखियाओं के माध्यम से आम जनता की जातिगत एकता के संस्कारों का लाभ उठाकर, उनके वोट आसानी से हासिल कर लिये जाते हैं। भारत के चुनाव विशेषज्ञों की सारी विशेषज्ञता इस बात में निहित होती है कि वे जातिगत सामाजिक समीकरणों को किस हद तक समझते हैं। टेलीविजन आधुनिकतम प्रौद्योगिकी-आधारित एक ऐसा माध्यम है जो जनमानस और सांस्कृतिक मूल्यों को बदलने में शायद सबसे प्रभावी भूमिका निभा सकता है। लेकिन टेलीविजन पर धार्मिक प्रचार के चैनलों की संख्या एक दर्जन के आसपास है, जबकि विज्ञान–तकनोलॉजी-वैज्ञानिक जीवन दृष्टि पर केन्द्रित एक भी चैनल नहीं हैं। न्यूज चैनलों से लेकर मनोरंजन के चैनलों तक सर्वाधिक सामग्री जादू-टोना, भूत-प्रेत, अन्धविश्वास, परम्परा-पूजा और रूढ़ियों के प्रचार से जुड़ी होती है।
इन सभी उदाहरणों के माध्यम से हम कहना यह चाहते हैं कि भारतीय समाज एक ऐसा विशिष्ट प्रकृति का पूँजीवादी समाज है जिसमें उत्पादन और विनिमय की प्रणाली के स्तर पर पूँजी का, बाज़ार का वर्चस्व स्थापित हो चुका है, पर इस विशिष्ट प्रकृति के पूँजीवाद ने अधिकांश प्राक्-पूँजीवादी मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं को तोड़ने के बजाय अपना लिया है तथा विविध रूपों में पूँजी और पूँजीवादी व्यवस्था की सेवा में सन्नद्ध कर दिया है। हमारे समाज में तमाम मध्ययुगीन स्वेच्छाचारी मूल्यों-मान्यताओं के साथ ही अलगाव, पण्यपूजा, व्यक्तिवाद और बुर्जुआ निरंकुशता जैसे पतनशील बुर्जुआ मूल्यों का एक विचित्र सहमेल मौजूद है। पुरानी बुराइयों के साथ नयी बुराइयों का यह सहअस्तित्व बुर्जुआ समाज के हर प्रकार के अन्याय को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करने का काम करता है। यह एक ऐसा बुर्जुआ समाज है जिसमें प्राक्-नागरिक समाज के मूल्यों-मान्यताओं का सहारा लेकर शोषक वर्ग शासित वर्ग में यह भ्रम पैदा करता है कि व्यवस्था उनकी सहमति (कन्सेण्ट) से चल रही है। इस रूप में शासक वर्ग शासित वर्गों पर अपना वर्चस्व, यानी सहयोजन के साथ प्रभुत्व, स्थापित करता है, जैसा कि प्रत्येक नागरिक समाज में होता है। इस वर्चस्व के जरिये बुर्जुआ राज्य की रक्षा होती है और अपनी पारी में, राज्य अपनी संस्थाओं के जरिए इस वर्चस्व को बनाये रखने में भूमिका निभाता है। यानी भारत का बुर्जुआ समाज एक ऐसा नागरिक समाज है, जिसमें शासक वर्ग के वर्चस्व को बनाये रखने में प्राक्-नागरिक समाज की अस्मिताओं-मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं की अहम भूमिका होती है। इन अर्थों में यहाँ की स्थिति यूरोपीय नागरिक समाजों से काफ़ी हद तक भिन्न है।
लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि वैचारिक-सांस्कृतिक स्तर पर आज प्राक्-नागरिक समाज के मूल्यों-मान्यताओं के विरुद्ध संघर्ष करके एक यूरोपीय ढंग के नागरिक समाज, (यानी बुर्जुआ समाज) के मूल्यों-मान्यताओं को स्थापित किया जा सकता है। इतिहास के इस दौर में यह सम्भव नहीं है। हम पीछे मुड़कर बुर्जुआ पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति की प्रक्रिया नये सिरे से शुरू नहीं कर सकते। इतिहास की विशिष्ट गति से आविर्भूत जो भी भारतीय बुर्जुआ समाज हमारे सामने मौजूद है, उसे नष्ट करके ही इसकी सभी बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है जिनमें मध्ययुगीन मूल्य-मान्यताएँ भी शामिल हैं। नये सिरे से एक आदर्श बुर्जुआ समाज नहीं बनाया जा सकता। वर्तमान बुर्जुआ समाज का विकल्प एक ऐसा समाज ही हो सकता है, जिसमें उत्पादन मुनाफ़े के लिए नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकताओं को केन्द्र में रखकर होता हो, जिसमें उत्पादन, राजकाज और समाज पर बहुसंख्यक उत्पादक जनसमुदाय का नियंत्रण कायम हो। ऐसे समाज में न केवल श्रम विभाजन, अलगाव और पण्यपूजा की संस्कृति नहीं होगी, बल्कि तर्कणा, जनवाद और व्यक्तिगत आज़ादी का निषेध करने वाली सभी मध्ययुगीन मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जायेगा। ज़ाहिर है कि यह सबकुछ एक झटके से नहीं हो जायेगा। राजनीतिक व्यवस्था-परिवर्तन और आर्थिक सम्बन्धों के परिवर्तन के साथ-साथ और उसके बाद भी सतत् समाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति की एक लम्बी प्रक्रिया के बाद ही ऐसा सम्भव हो सकेगा।
हरेक राजनीतिक आन्दोलन की पूर्ववर्ती, सहवर्ती और अनुवर्ती सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन की स्वयंस्फ़ूर्त धाराएँ अनिवार्यतः उपस्थित होती हैं। लेकिन इन सहवर्ती-अनुवर्ती धाराओं की स्वयंस्फ़ूर्त गति एवं परिणति पर नियतत्ववादी ढंग से ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिए। यानी, यह मानकर नहीं चला जाना चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्था-परिवर्तन और आर्थिक सम्बन्धों के बदलने के साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक अधिरचनात्मक तंत्र भी स्वतः बदल जायेगा। आर्थिक मूलाधार से आविर्भूत-निर्धारित होने के बावजूद अधिरचना की अपनी सापेक्षतः स्वतंत्र गति होती है और उसे बदलने के लिए अधिरचना के धरातल पर भी सचेतन प्रयास की, अधिरचना में क्रान्ति की आवश्यकता होती है। राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलनों को जन्म और गति देती है और साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को मज़बूत, गतिमान और गहरा बनाते हैं। भारत में औपनिवेशिक दौर, राष्ट्रीय आन्दोलन और उसके बाद पूँजीवादी समाज विकास का जो विशिष्ट इतिहास रहा, आज के समाज में मध्ययुगीन मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं की मौजूदगी उसी का एक प्रतिफ़ल है। जो काम राष्ट्रीय जनवादी क्रान्ति के दौर में हो सकता था, वह नहीं हुआ। सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ता किंचित सुगबुगाहट और ऊपरी बदलावों के बावजूद बनी रही। अब एक प्रबल वेगवाही सामाजिक झंझावात ही इस जड़ता को तोड़कर भारतीय समाज की शिराओं में एक नयी ऊर्जस्विता और संवेग का संचार कर सकता है। यह तफ़ूान पूँजीवादी सामाजिक-आर्थिक संरचना और राजनीतिक व्यवस्था के साथ ही उन सभी नये-पुराने मूल्यों और संस्थाओं को भी अपना निशाना बनायेगा जो इस व्यवस्था से सहारा पाते हैं और इसे सहारा देते हैं।
प्रेम की आज़ादी के प्रश्न को भी इसी ऐतिहासिक-सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में देखा-समझा जा सकता है। व्यक्तिगत और खण्डित संघर्ष इस प्रश्न को एजेण्डा पर उपस्थित तो कर सकते हैं, लेकिन हल नहीं कर सकते। सामाजिक ताने-बाने में जनवाद और व्यक्तिगत आज़ादी के अभाव और मध्ययुगीन कबीलाई, निरंकुश स्वेच्छाचारिता के प्रभुत्व को तोड़े बिना, परम्पराओं और रूढ़ियों की जकड़बन्दी को छिन्न-भिन्न किये बिना, प्रेम की आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए यह सवाल एक आमूलगामी सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति का सवाल है। हमें भूलना नहीं होगा कि प्रेम और जीवन–साथी चुनने की आज़ादी का प्रश्न जाति प्रश्न और स्त्री-प्रश्न से तथा धार्मिक आधार पर कायम सामाजिक पार्थक्य की समस्या से बुनियादी रूप से जुड़ा हुआ है। इन प्रश्नों पर एक व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन ही समस्या के अन्तिम हल की दिशा में जाने वाला एकमात्र रास्ता है। और साथ ही, इसके बिना, राजनीतिक व्यवस्था-परिवर्तन की किसी लड़ाई को भी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जा सकता। जो समाज अपनी युवा पीढ़ी को अपनी ज़िन्दगी के बारे में बुनियादी फ़ैसले लेने तक की इजाज़त नहीं देता, जहाँ परिवार में पुरानी पीढ़ी और पुरुषों का निरंकुश स्वेच्छाचारी अधिनायकत्व आज भी प्रभावी है, जिस समाज के मानस पर रूढ़ियों-परम्पराओं की आक्टोपसी जकड़ कायम है, वह समाज बुर्जुआ समाज के सभी अन्याय-अनाचार को और बुर्जुआ राज्य के वर्चस्व को स्वीकारने के लिए अभिशप्त है। इसीलिए, कोई आश्चर्य नहीं कि संविधान और क़ानून की किताबों में व्यक्तिगत आज़ादी और जनवाद की दुहाई देने वाली बुर्जुआ राज्यसत्ता अपने तमाम प्रचार–माध्यमों के जरिए धार्मिक-जातिगत रूढ़ियों-मान्यताओं, अन्धविश्वासों और मध्ययुगीन मूल्यों को बढ़ावा देने का काम करती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वह जनसमुदाय से अपने शासन के लिए एक किस्म की "स्वयंस्फ़ूर्त"सहमति हासिल करती है और यह भ्रम पैदा करती है कि उसका प्रभुत्व जनता की सहमति से कायम है। जो समाज भविष्य के नागरिकों को रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह करने की इजाज़त नहीं देता, वह अपनी गुलामी की बेड़ियों को खुद ही मज़बूत बनाने का काम करता है। इन्हीं रूढ़ियों-परम्पराओं के ऐतिहासिक कूड़े-कचरे के ढेर से वे फ़ासिस्ट गिरोह खाद-पानी पाते हैं जो मूलतः एक असाध्य संकटग्रस्त बुर्जुआ समाज की उपज होते हैं। "अतीत के गौरव"की वापसी का नारा देती हुई ये फ़ासिस्ट शक्तियाँ वस्तुतः पूँजी के निरंकुश सर्वसत्तावादी शासन की वकालत करती हैं और धार्मिक-जातिगत-नस्ली-लैंगिक रूढ़ियों को मज़बूत बनाकर व्यवस्था की बुनियाद को मज़बूत करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। बाबू बजरंगी और प्रेमी जोड़ों पर हमले करने वाले गुण्डा गिरोह इन्हीं शक्तियों के प्रतिनिधि उदाहरण हैं।
प्रेम की आज़ादी का सवाल रूढ़ियों के विद्रोह का प्रश्न है। यह जाति-प्रथा के विरुद्ध भी विद्रोह है। सच्चे अर्थों में प्रेम की आज़ादी का प्रश्न स्त्री की आज़ादी के प्रश्न से भी जुड़ा है, क्योंकि प्रेम आज़ाद और समान लोगों के बीच ही वास्तव में सम्भव है। प्रेम के प्रश्न को हम सामाजिक-आर्थिक मुक्ति के बुनियादी प्रश्न से अलग काटकर नहीं देख सकते। सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति के एजेण्डा से हम इस प्रश्न को अलग नहीं कर सकते। इस प्रश्न को लेकर हमारे समाज में संघर्ष के दो रूप बनते हैं। एक, फ़ौरी तथा दूसरा दूरगामी। फ़ौरी तौर पर, जब भी कहीं कोई बाबू बजरंगी या धार्मिक कट्टरपंथियों का कोई गिरोह या कोई जाति-पंचायत प्रेमी जोड़ों को जबरन अलग करती है या कोई सज़ा सुनाती है, तो यह व्यक्तिगत आज़ादी या जनवादी अधिकार का एक मसला बनता है। इस मसले को लेकर क्रान्तिकारी छात्र-युवा संगठनों, सांस्कृतिक संगठनों, नागरिक अधिकार संगठनों आदि को आगे आना चाहिए और रस्मी कवायदों से आगे बढ़कर प्रतिरोध की संगठित आवाज़ उठानी चाहिए, संविधान और क़ानून रस्मी तौर पर हमें जो अधिकार देते हैं उनका भी सहारा लेना चाहिए और व्यापक आम जनता के बीच अपनी बात ले जाकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यह प्रक्रिया युवा समुदाय और समाज के प्रबुद्धतत्वों की चेतना को 'रैडिकलाइज़'करने का भी काम करेगी। लेकिन मात्र इसी उपक्रम को समस्या का अन्तिम समाधान मान लेना एक सुधारवादी दृष्टिकोण होगा। यह केवल फ़ौरी कार्यभार ही हो सकता है। इसके साथ एक दूरगामी कार्यभार भी है और वही फ़ौरी कार्यभार को भी एक क्रान्तिकारी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। प्रेम की आज़ादी का प्रश्न बुनियादी तौर पर समाज के मौजूदा आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक ढाँचे के क्रान्तिकारी परिवर्तन से जुड़ा हुआ है और इस रूप में यह बुर्जुआ समाज-विरोधी नयी मुक्ति-परियोजना का एक अंग है। जातिगत-धार्मिक रूढ़ियों से मुक्ति और स्त्रियों की आज़ादी के प्रश्न से भी यह अविभाज्यतः जुड़ा हुआ है। इस रूप में इस समस्या का हल एक दीर्घकालिक संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के बिना सम्भव नहीं। व्यवस्था-परिवर्तन के क्रान्तिकारी संघर्ष की कड़ियों के रूप में संगठित युवाओं के आन्दोलन, सांस्कृतिक आन्दोलन, स्त्री-आन्दोलन और नागरिक अधिकार आन्दोलन की एक लम्बी और जुझारू प्रक्रिया ही इस समस्या के निर्णायक समाधान की दिशा में भारतीय समाज को आगे ले जा सकती है। यही नहीं, व्यवस्था-परिवर्तन के बाद भी समाज की हरावल शक्तियों को सामाजिक-सांस्कृतिक अधिरचना में सतत् क्रान्ति की दीर्घकालिक प्रक्रिया चलानी होगी, तभी सच्चे अर्थों में समानता और आज़ादी की सामाजिक व्यवस्था कायम होने के साथ ही रूढ़ियों की दिमाग़ी गुलामी से और मानवद्रोही पुरातनपंथी मूल्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व से छुटकारा मिल सकेगा और सच्चे अर्थों में आदर्श मानवीय प्रेम को ज़िन्दगी की सच्चाई बनाया जा सकेगा, जो कम से कम आज, सुदूर भविष्य की कोई चीज़ प्रतीत होती है।
प्रेम, परम्परा और विद्रोह
कात्यायनी
(दूसरी किश्त)
अब इस प्रश्न के एक और पहलू पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए। चाहे अन्तर्जातीय-अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले किसी युवा जोड़े पर जाति-बिरादरी के पंचों द्वारा बर्बर अत्याचार का सवाल हो, चाहे एम.एफ़.हुसैन के चित्रों के विरुद्ध हिन्दुत्ववादी फ़ासिस्टों की मुहिम हो, या चाहे नागरिक अधिकार, जनवादी अधिकार और व्यक्तिगत आज़ादी से जुड़ा कोई भी मसला हो, इन सवालों पर पढ़े-लिखे मध्यवर्ग का या आम छात्रों-युवाओं का भी बड़ा हिस्सा संगठित होकर सड़कों पर नहीं उतरता। ऊपर हमने इसके सामाजिक-ऐतिहासिक कारणों की आम चर्चा की है। लेकिन उस आम कारण के एक विशिष्ट विस्तार पर भी चर्चा ज़रूरी है, जो आज के भारतीय समाज में प्रगतिशील एवं जनवादी माने जाने वाले बुद्धिजीवियों की स्थिति और आम जनता के विभिन्न वर्गों के साथ उनके रिश्तों से जुड़ी हुई है।
जब भी अन्तर्जातीय-अन्तर्धार्मिक प्रेम या विवाह करने वाले किसी जोड़े पर अत्याचार की या नागरिक अधिकार के हनन की कोई घटना सामने आती है तो दिल्ली या किसी राज्य की राजधानी या किसी अन्य महानगर की सड़कों पर कुछ थोड़े से मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी उसके प्रतीकात्मक विरोध के लिए आगे आते हैं। (दिल्ली में) मण्डी हाउस से होकर जन्तर मन्तर तक, कहीं भी कुछ लोग धरने पर बैठ जाते हैं, किसी एक शाम को मोमबत्ती जुलूस या मौन जुलूस निकाल दिया जाता है, एक जाँच दल घटना-स्थल का दौरा करने के बाद वापस आकर प्रेस के लिए और बुद्धिजीवियों के बीच सीमित वितरण के लिए एक रिपोर्ट जारी कर देता है और कुछ जनहित याचिकाएँ दाखिल कर दी जाती हैं। इन सभी कार्रवाइयों का दायरा अत्यन्त सीमित और अनुष्ठानिक होता है। इनका कर्ता-धर्ता जो बुद्धिजीवी समुदाय होता है, वह केवल तात्कालिक और संकुचित दायरे की इन गतिविधियों से अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री करके अपने प्रगतिशील और जनवादी होने का "प्रमाण"प्रस्तुत कर देता है। व्यापक आम आबादी तक अपनी बात पहुँचाने का, प्रचार और उद्वेलन की विविधरूपा कार्रवाइयों द्वारा उसे जागृत और संगठित करने का तथा ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सामाजिक-सांस्कृतिक आन्दोलन संगठित करने का कोई दूरगामी-दीर्घकालिक कार्यक्रम उनके एजेण्डे पर वस्तुतः होता ही नहीं। उनकी अपेक्षा केवल सत्ता से होती है कि वह संवैधानिक प्रावधनों-क़ानूनों का सहारा लेकर प्रतिक्रियावादी सामाजिक-राजनीतिक ताकतों के हमलों से आम लोगों के जनवादी अधिकारों और व्यक्तिगत आज़ादी की हिफ़ाजत सुनिश्चित करे। लोकतंत्र के मुखौटे को बनाये रखने के लिए सरकार और प्रशासन तंत्र भी कुछ रस्मी कार्रवाई करते हैं, कभी-कभार कुछ जाँच, कुछ गिरफ्तारियाँ होती हैं और कुछ क़ानूनी कार्रवाइयाँ भी शुरू होती हैं और फ़िर समय बीतने के साथ ही सब कुछ ठण्डा पड़ जाता है।
दरअसल सत्ता और सभी पूँजीवादी चुनावी दलों के सामाजिक अवलम्ब ज़मीनी स्तर पर वही प्रतिगामी और रूढ़िवादी तत्व होते हैं, जो सामाजिक स्तर पर जाति-उत्पीड़न, स्त्री-उत्पीड़न और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अलगाव एवं उत्पीड़न के सूत्रधार होते हैं। इसलिए हमारे देश की बुर्जुआ सत्ता यदि चाहे भी तो उनके विरुद्ध कोई कारगर क़दम नहीं उठा सकती। यदि उसे सीमित हद तक कोई प्रभावी क़दम उठाने के लिए मज़बूर भी करना हो तो व्यापक जन-भागीदारी वाले किसी सामाजिक आन्दोलन के द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है। इससे भी अहम बात यह है कि ऐसा कोई सामाजिक आन्दोलन सत्ता के क़दमों और क़ानूनों का मोहताज़ नहीं होगा, वह स्वयं नये सामाजिक मूल्यों को जन्म देगा, जनमानस में उन्हें स्थापित करेगा और रूढ़िवादी शक्तियों एवं संस्थाओं के वर्चस्व को तोड़ने की आमूलगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ायेगा। इस काम को वह बुद्धिजीवी समाज कत्तई अंजाम नहीं दे सकता जो प्रगतिशील, वैज्ञानिक और जनवादी मूल्यों का आग्रही तो है, लेकिन समाज में उन मूल्यों को स्थापित करने के लिए न तो कोई तकलीफ़ झेलने के लिए तैयार है और न ही कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार है।
जो बुद्धिजीवी आज वामपंथी, प्रगतिशील, सेक्युलर और जनवादी होने का दम भरते हैं तथा तमाम रस्मी एवं प्रतीकात्मक कार्रवाइयों में लगे रहते हैं, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर निगाह डालने से बात साफ़ हो जायेगी। प्रायः ये महानगरों में रहने वाले विश्वविद्यालयों-कालेजों के प्राध्यापक, मीडियाकर्मी, वकील, फ्रीलांसर पत्रकार व लेखक तथा एन.जी.ओ. व सिविल सोसाइटी संगठनों के कर्त्ता-धर्ता हैं। कुछ थोड़े से डॉक्टर, इंजीनियर जैसे स्वतंत्र प्रोफेशनल्स और नौकरशाह भी इनमें शामिल हैं जो प्रायः प्रगतिशील लेखक या संस्कृतिकर्मी हुआ करते हैं। आर्थिक आय की दृष्टि से इनमें से अधिकांश का जीवन सुरक्षित है, इनकी एक सामाजिक हैसियत और इज्ज़त है। यह कथित प्रगतिशील जमात आज़ादी के बाद की आधी सदी, विशेषकर पिछले लगभग तीन दशकों के दौरान, तेज़ी से सुख-सुविधा सम्पन्न हुए मध्यवर्ग की उस ऊपरी परत का अंग बन चुकी है, जिसे इस पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर आर्थिक सुरक्षा के साथ ही सामाजिक हैसियत की बाड़ेबन्दी की सुरक्षा और जनवादी अधिकार भी हासिल हैं। इस सुविधासम्पन्न विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक उपभोक्ता वर्ग में प्रोफेसर, मीडियाकर्मी, वकील आदि के रूप में रोज़ी कमाने वाले जो प्रगतिशील लोग शामिल हैं, वे अपने निजी जीवन में यदि जाति-धर्म को नहीं मानते हैं, स्वयं प्रेम विवाह करते हैं, अपने बच्चों को इसकी इजाज़त देते हैं और प्रगतिशील आचरण करते हैं, तो भी वे इन मूल्यों को व्यापक आम आबादी के बीच ले जाने के लिए किसी सामाजिक-सांस्कृतिक मुहिम का भागीदार बनने की जहमत या जोखिम नहीं उठाते। साथ ही, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो प्रगतिशीलता की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी निजी व पारिवारिक ज़िन्दगी में निहायत पुराणपंथी हैं। चुनावी वामपंथी दलों के नेताओं में से अधिकांश ऐसे ही हैं। इनमें से पहली कोटि के प्रगतिशीलों का कुलीनतावादी जनवाद और वामपंथ हो या दूसरी कोटि के प्रगतिशीलों का दोगला-दुरंगा जनवाद और वामपंथ-मेहनतकश और सामान्य मध्यवर्ग के लोग उन्हें भली-भाँति पहचानते हैं और उनसे घृणा करते हैं। कुलीनतावादी प्रगतिशीलों और छद्म वामपंथियों का जीवन मुख्य तौर पर देश के ऊपरी पन्द्रह-बीस करोड़ आबादी के जीवन का हिस्सा बन चुका है, उस उच्च मध्यवर्गीय आबादी का हिस्सा बन चुका है जो एक लम्बी पीड़ादायी क्रमिक प्रक्रिया में, विकृत और आधे-अधूरे ढंग से, पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति के कार्यभारों के पूरा होने के बाद, आम जनसमुदाय के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात कर चुका है। उसे देश की लगभग पचपन करोड़ सर्वहारा-अर्द्धसर्वहारा आबादी या रोजाना बीस रुपये से कम पर जीने वाली चौरासी करोड़ आबादी के जीवन के अँधेरे और यंत्रणाओं से अब कुछ भी लेना-देना नहीं रह गया है। एक परजीवी जमात के रूप में वह मेहनतकशों से निचोड़े गये अधिशेष का भागीदार बन चुका है। आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से इस परजीवी वर्ग का हिस्सा बन चुके जो बुद्धिजीवी प्रगतिशील, जनवादी और सेक्युलर विचार रखते हैं, उनकी कुलीनतावादी, अनुष्ठानिक, नपुंसक प्रगतिशीलता आम लोगों में घृणा और दूरी के अतिरिक्त भला और कौन सा भाव पैदा कर सकती है? इस तबके की जो स्त्रियाँ हैं, ऊपरी तौर पर आमलोगों को वे आज़ाद लगती हैं (हालाँकि वस्तुतः ऐसा होता नहीं) और यह आज़ादी उनकी विशेष सुविधा प्रतीत होती है जिसके चलते मेहनतकश और आम मध्यवर्ग की स्त्रियाँ (ऊपर से सम्मान देती हुई भी) उनसे बेगानगी या घृणा तक का भाव महसूस करती हैं तथा उन्हें अपने से एकदम अलग मानती हैं।
उपरोक्त पूरी चर्चा के जरिए हम इस सच्चाई की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि प्रेम करने की आज़ादी पर रोक सहित किसी भी मध्ययुगीन बर्बरता, धार्मिक कट्टरपंथी हमले या जातिवादी उत्पीड़न के विरुद्ध कुलीनतावादी प्रगतिशीलों की रस्मी, प्रतीकात्मक कार्रवाइयों का रूढ़िवादी शक्तियों और मूल्यों पर तो कोई असर नहीं ही पड़ता है, उल्टे आम जनता पर भी इनका उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। सुविधासम्पन्न, कुलीनतावादी प्रगतिशीलों का जीवन आम लोगों से इतना दूर है कि उनके जीवन–मूल्य (यदि वास्तविक हों तो भी) जनता को आकृष्ट नहीं करते।
एक दूसरी बात जो ग़ौरतलब है, वह यह कि आज के भारतीय समाज में मध्ययुगीन बुराइयों के साथ-साथ आधुनिक बुर्जुआ जीवन की तमाम बुराइयाँ और विकृतियाँ भी मौजूद हैं। आम लोगों को पुरानी बुराइयों के विकल्प के तौर पर समाज में आधुनिक बुर्जुआ जीवन की बुराइयाँ ही नज़र आती हैं। पुरानी बुराइयों के साथ जीने की उन्हें आदत पड़ चुकी है। उनसे उनका परिचय पुराना है। इसलिए नई बुराइयाँ उन्हें ज्यादा भयावह प्रतीत होती हैं। आधुनिक बुर्जुआ जीवन की सामाजिक-सांस्कृतिक विकृतियों को देखकर वे पुराने जीवन–मूल्यों से चिपके रहने का स्वाभाविक विकल्प चुनते हैं। महानगरों में तरह-तरह के सेक्स रैकेट्स, प्रेम विवाहों की विफलता, यौन अपराधों आदि की खबरें पढ़-सुनकर और मीडिया में बढ़ती अश्लीलता आदि देखकर आम नागरिक इन्हें आधुनिक जीवन का प्रतिफ़ल मानते हैं और इनसे सहज प्रतिक्रियास्वरूप उन रूढ़ियों को अपना शरण्य बनाते हैं जिनके साथ जीने के वे शताब्दियों से और पीढ़ियों से आदि रहे हैं। इसका एक वस्तुगत कारण आज की ऐतिहासिक-सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों में भी मौजूद है, जब प्रगति की धारा पर विपर्यय और प्रतिगामी पुनरुत्थान की धारा हावी है और चतुर्दिक गतिरोध का माहौल है। और मनोगत कारण यह है कि विपर्यय और गतिरोध के इस दौर में ऐतिहासिक परिवर्तन की वाहक मनोगत शक्तियाँ अभी बिखरी हुई और निहायत कमज़ोर हैं। नये सिरे से नयी ज़मीन पर उनके उठ खड़े होने की प्रक्रिया अभी एकदम शुरुआती दौर में है। ऐसी ही शक्तियाँ अपने विचार और व्यवहार के द्वारा जनता के सामने मध्ययुगीन और विकृत बुर्जुआ जीवन मूल्यों का नया, मानवीय और वैज्ञानिक विकल्प प्रस्तुत कर सकती हैं।
फ़िलहाल की गतिरुद्ध स्थिति के बारे में भगतसिंह का उद्धरण एकदम सटीक ढंग से लागू होता है और ऐसी स्थिति में नयी क्रान्तिकारी शक्तियों के दायित्व के बारे में भी यह एकदम सही बात कहता है: "जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो किसी भी प्रकार की तब्दीली से वे हिचकिचाते हैं। इस जड़ता और निष्क्रियता को तोड़ने के लिए एक क्रान्तिकारी स्पिरिट पैदा करने की ज़रूरत होती है, अन्यथा पतन और बर्बादी का वातावरण छा जाता है। लोगों को गुमराह करने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ जनता को ग़लत रास्ते पर ले जाने में सफ़ल हो जाती हैं। इससे इंसान की प्रगति रुक जाती है और उसमें गतिरोध आ जाता है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यह ज़रूरी है कि क्रान्ति की स्पिरिट ताज़ा की जाए, ताकि इंसानियत की रूह में हरकत पैदा हो।
जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है, सच्चे अर्थों में दो स्त्री-पुरुष नागरिकों के बीच प्रेम की आज़ादी का प्रश्न इतिहास का एक दीर्घकालीन प्रश्न है। केवल पुरातन मध्ययुगीन रूढ़ियाँ, जाति और धर्म के बन्धन और बड़े-बुजुर्गों का निरंकुश स्वेच्छाचारी वर्चस्व ही प्रेम करने की मानवीय आज़ादी के राह की बाधाएँ नहीं हैं। जिस समाज में पूँजी का जीवन पर चतुर्दिक वर्चस्व स्थापित हो, उस समाज में मनुष्य की तमाम आज़ादियों के साथ ही प्रेम करने की आज़ादी पर भी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में, स्थूल और सूक्ष्म रूप में, प्रेम की स्वतंत्रता पर एक हज़ार एक पाबन्दियाँ अनिवार्यतः काम करती रहती हैं। पूँजीवादी समाज में जो उजरती गुलाम हडि्डयाँ गलाकर भी महज इतना ही हासिल कर पाते हैं कि उत्पादन करने के लिए बस जीवित रह सके और उजरती गुलामों की नयी पीढ़ी पैदा कर सकें, जिनके पास आत्मीयता और सुकून के पल गुजारने के लिए न समय होता है न पैसा और जो मनुष्यता के सभी आत्मिक-सांस्कृतिक सम्पदा से अपरिचित होते हैं, उनके लिए प्रेम की आज़ादी का भला क्या अर्थ हो सकता है? पूँजी से पूँजी बटोरना ही जिन पूँजीपतियों का जीवन होता है और पूँजी स्वयं जिन पर जीन–लगाम कसकर सवारी करती रहती है, वे पूँजीपति प्यार करने के मिथ्याभास में जीने के अतिरिक्त भला क्या कर सकते हैं? जिस समाज में तमाम जनवादी अधिकारों और समानताओं के दावों के बावजूद स्त्रियाँ दोयम दर्जे की नागरिक हों, वहाँ भला सच्चे अर्थों में प्रेम कैसे सम्भव हो सकता है, क्योंकि यह तो सच्चे अर्थों में आज़ाद और समान नागरिकों के बीच ही सम्भव हो सकता है। और सबसे बुनियादी प्रश्न यह है कि जिस समाज में पण्य पूजा (कमोडिटी फ़ेटिसिज्म) सामाजिक-श्रम विभाजन से पैदा हुए अलगाव (एलियनेशन), 'रीइफ़िकेशन', आत्म-निर्वासन और व्यक्तित्व के विघटन ने आम नागरिकों को मानवीय मूल्यों और मानवीय सारतत्व से बेगाना बना दिया है, उस समाज में प्रेम की आज़ादी क्या एक वस्तुगत यथार्थ हो सकता है? यूरोप के प्रबोधन-कालीन दार्शनिकों और बुर्जुआ जनवादी क्रान्तियों ने स्त्री-पुरुष समानता और व्यक्तिगत आज़ादी के उसूलों पर आधारित एकनिष्ठ या एकान्तिक प्रेम के जिस स्वरूप को और उसकी आज़ादी को उन्नत मानव जीवन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया और जिसने सीमित हद तक यूरोप के प्रारम्भिक बुर्जुआ जीवन में कुछ स्वस्थ-सकारात्मक मूल्य भी पैदा किये, हम उसके ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन बुर्जुआ सामाजिक ढाँचे और श्रम-विभाजन के जड़ीभूत होने के साथ ही उसका अग्रवर्ती विकास रुक गया, प्रबोधनकालीन आदर्श स्खलित हो गये और फ़िर बीसवीं शताब्दी के ह्रासमान पूँजीवाद ने मनुष्यता को आत्मिक वंचना और मानवद्रोही संस्कृति के वर्चस्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया। प्रबोधनकालीन आदर्शों के परचम को फ़िर पूँजीवाद-विरोधी सर्वहारा क्रान्ति की विचारधारा ने ऊँचा उठाया और उसी ने पहली बार यह विचार प्रस्तुत किया कि प्रेम की पूर्ण स्वतंत्रता केवल उसी समय आम तौर पर स्थापित हो सकेगी जब पूँजीवादी उत्पादन, उससे उत्पन्न स्वामित्व-सम्बन्ध और आत्मिक मूल्य समाप्त हो जायेंगे। यह एक सुदूर भविष्य की बात है, लेकिन जो इतिहास की वर्तमान अवस्था को ही इसका अन्त नहीं मानते, सच्चे मानवीय प्रेम के बारे में आज उनका यही आदर्श हो सकता है और यही भविष्य-स्वप्न हो सकता है। लेख के इस हिस्से में हम इसी विषय पर कुछ विस्तार से विचार करेंगे। प्रेम की अवधारणा की शाश्वतता और अलौकिकता के मिथक को खण्डित करने के लिए और इसकी वास्तविकता को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐतिहासिक-सामाजिक विवेचना के थोड़े विस्तार में जायें। इस प्रसंग से लेख के इस हिस्से में थोड़ी सी दार्शनिक जटिलता भी आ सकती है, लेकिन इस अपरिहार्य विवशता के लिए पाठक हमें क्षमा करेंगे।
बात हमने इस प्रसंग में शुरू की थी कि यदि प्रेम करने की आज़ादी की बात करते हुए हम केवल पुरातन मध्ययुगीन स्वेच्छाचारिता और रूढ़ियों-मूल्यों के विरुद्ध विद्रोह की ही बात करते हैं, तो यह मात्र एक बुर्जुआ जनवादी माँग होगी और इतिहास आज उस युग से काफ़ी दूर निकल आया है। आज भौतिक जीवन के साथ ही आत्मिक जीवन पर भी स्थापित पूँजी की मानवद्रोही वर्चस्ववादी सत्ता से मुक्ति के प्रश्न पर सोचे बिना मनुष्य की किसी भी प्रकार की आज़ादी की बात करना बेमानी है और इसमें प्रेम करने की आज़ादी भी शामिल है। (आगे हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि "प्रेम करने की आज़ादी"को बुर्जुआ अराजकतावादी अनैतिक मानस किस चश्मे से देखता है और इसका वास्तविक कम्युनिस्ट अर्थ क्या होता है)। यदि हम केवल प्रेम करने के किसी व्यक्ति की आज़ादी पर मध्ययुगीन रूढ़ियों-मूल्यों की बन्दिशों और उनके विरुद्ध विद्रोह की बात तक ही रुक जायेंगे तो यह बुर्जुआ प्रेम का आदर्शीकरण होगा। अतः हमें इससे आगे जाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रेम की अवधारणा को ही वृहत्तर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें। पश्चिम के जिन उन्नत बुर्जुआ समाजों में दो युवाओं के प्रेम करने या जीवन–साथी चुनने में रूढ़ियों-मूल्यों या बुजुर्गों का हस्तक्षेप न के बराबर रह गया है, क्या कारण है कि वहाँ भी विवाहेतर सम्बन्धों, बेवफ़ाई, बलात्कार, स्त्री-उत्पीड़न तथा नीरस घिसटते और टूटते वैवाहिक जीवन की घटनाएँ इतनी आम हो चुकी हैं कि सामाजिक ताना-बाना ही टूटता-बिखरता प्रतीत होता है। समृद्धि और प्रेम करने की प्रतीयमान या औपचारिक आज़ादी के बावजूद अवसाद और तमाम प्रकार की मनोविकृतियों से पश्चिमी समाज इस कदर ग्रस्त क्यों है? कारण एकदम स्पष्ट है। दो मनुष्य किसी द्वीप पर रहकर प्यार नहीं करते। वे इसी समाज में प्रेम करते हैं और उनका प्रेम भौतिक जीवन स्थितियों और सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश एवं मूल्यों से स्वतंत्र, अछूता, निरपेक्ष नहीं हो सकता।
एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्यों के बीच प्रेम कोई जैविक आवेग, ईश्वरीय वरदान या समाज-निरपेक्ष भावना नहीं होता। प्रेम की अवधारणा सामाजिक वर्गीय संरचना से स्वतंत्र, शाश्वत और विविक्त नहीं होती। जिस प्रकार वर्ग समाज में जेण्डर एक जैविक तथ्य से भी कहीं अधिक एक 'सोशल कंस्ट्रक्ट'है, उसी प्रकार स्त्री-पुरुष के बीच का प्रेम भी एक 'सोशल कंस्ट्रक्ट'है। यह एक सामाजिक-विचारधारात्मक-सांस्कृतिक अवधारणा है जो सामाजिक संरचना और आत्मिक मूल्यों में बदलाव के साथ बदलती रही है। प्रेम और प्रेम करने की आज़ादी के निहितार्थ की वर्ग-सापेक्षता और काल-सापेक्षता को समझने के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है। इसके लिए हम स्त्री-पुरुष के बीच प्रेम की अवधारणा की ऐतिहासिक विकास-प्रक्रिया का यहाँ संक्षिप्त उल्लेख करेंगे।
कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक 'दर्शन की दरिद्रता'में लिखा है: 'मानव प्रकृति का सतत रूपान्तरण ही इतिहास है' ('द पावर्टी ऑफ़ फ़िलॉसोफी', इण्टरनेशनल पब्लिशर्स, न्यूयार्क, 1963, पृ- 147) मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जिसकी यह प्रकृति है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करता है। जब वह ऐसा नहीं करता था तो पशुजगत का एक अंग था। फ़िर श्रम की विशिष्टता ने उसे मनुष्य बनाया (देखिए, फ्रेडरिक एंगेल्स: 'वानर से नर बनने में श्रम की भूमिका')। जैविक आवश्यकताओं से प्रेरित पाशविक सम्भोग से विच्छेद कर आगे बढ़ने की ज़मीन भी तभी तैयार हुई, जब पशुजगत से बाहर संक्रमण करके मनुष्य ने प्रकृति से पहला निर्णायक विच्छेद किया और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू किया। अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह प्रकृति-प्रदत्त चीज़ों पर निर्भर रहने के बजाय काम करने लगा, यानी अपने श्रम से, प्राकृतिक चीज़ों से कुछ नयी चीज़ों का निर्माण करने लगा। यह एक सामूहिक प्रक्रिया थी, यानी श्रम की सारवस्तु शुरू से ही सामाजिक थी। अपने उद्गम और मूल प्रकृति से ही मनुष्य का सारतत्व अलग-थलग व्यक्तित्वों पर आधारित अमूर्तन नहीं है। मानवीय अस्तित्व श्रम पर आधारित और ऐतिहासिक विकास-प्रक्रिया से गुजरने वाले सामाजिक सम्बन्धों के समुच्चय के अन्तर्गत, और इसके द्वारा, संघटित हुआ है। कहा जा सकता है कि मनुष्य का जीवन अपने स्वत्व और उसके लिए ज़रूरी भौतिक वस्तुओं को अर्जित करने और फ़िर उस स्थिति का अतिक्रमण करके आगे बढ़ने की एक सतत् प्रक्रिया है जो उसकी चेतना, भावनाओं और आत्मिक जगत को भी निरन्तर समृद्ध बनाती रहती है। सभ्यता के इतिहास में, इसी प्रक्रिया में भौतिक उत्पादन के लिए ज़रूरी साहचर्य और मानवीय पुनरुत्पादन के लिए ज़रूरी सम्भोग-क्रिया ने सामाजिक संरचना और परिवार संस्था के विविध विकासमान रूपों के अन्तर्गत स्त्री-पुरुष की मानवीय चेतना में एक विशिष्ट आकर्षण की भावना को-एक विशिष्ट भावावेग को जन्म दिया जो सहस्त्राब्दियों से गुजरकर, आधुनिक, रोमानी, एकनिष्ठ (या एकान्तिक) यौन–प्रेम के रूप में विकसित हुआ।
मार्क्स और एंगेल्स अपनी पुस्तक 'जर्मन विचारधारा'में अत्यन्त तर्कसंगत ढंग से बताते हैं कि सभ्यता के विकास की तीन प्रारम्भिक स्थितियाँ और शर्तें रही हैं। पहली ऐतिहासिक शर्त और स्थिति रही है, भोजन, वस्त्र, आवास और अन्य ज़रूरतों की पूर्ति के साधनों का उत्पादन करना। दूसरी ऐतिहासिक शर्त और स्थिति यह रही है कि पहली आवश्यकता की पूर्ति (आवश्यकता-पूर्ति की क्रिया और उसके लिए अर्जित उपकरण) नयी आवश्यकताएँ पैदा कर देती हैं। ये दो शर्तें या स्थितियाँ मिलकर "पहला ऐतिहासिक कार्य"बन जाती हैं और इनके साथ एक तीसरी पूर्वशर्त-'एक तीसरे किस्म का प्राकृतिक-सामाजिक सम्बन्ध'-जुड़ जाती है। यह तीसरी स्थिति या शर्त, जो ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में शुरू में ही प्रविष्ट हो जाती है, यह है कि मनुष्य जो प्रतिदिन अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हैं, वे अपनी जाति को बढ़ाने के लिए दूसरे मनुष्यों का भी निर्माण करते हैं: यानी स्त्री-पुरुष के बीच सम्बन्ध का, अभिभावक और बच्चों के बीच सम्बन्ध का, परिवार का निर्माण करते हैं। यह परिवार शुरू में तो एकमात्र सामाजिक सम्बन्ध था, पर नयी-नयी पैदा होने वाली आवश्यकताओं द्वारा नये सामाजिक सम्बन्धों को जन्म देने और बढ़ती आबादी के चलते नयी-नयी आवश्यकताओं के पैदा होने के बाद यह एक अधीनस्थ सामाजिक सम्बन्ध बनकर रह गया। मार्क्स ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये तीन ऐतिहासिक शर्तें या स्थितियाँ तीन अलग-अलग अवस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि सभ्यता के उषाकाल से ही सामाजिक गतिविधि के तीन पहलुओं के रूप में मौजूद रही हैं और इतिहास के वर्तमान दौर में भी इनकी यही भूमिका है। (विस्तार के लिए देखें, मार्क्स और एंगेल्स: 'जर्मन आइडियोलॉजी', पृ- 31 और पृ- 39–41, प्रोग्रेस पब्लिशर्स, मास्को, 1964)
मनुष्य का इतिहास एक ही साथ, प्राकृतिक और सामाजिक दोनों है। जो स्थितियाँ और सम्बन्ध इसे जन्म देते हैं, उनके मूल में दोहरा उत्पादन होता है: श्रम के द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन और प्रजनन के द्वारा मानव जीवन का उत्पादन। मनुष्य प्रकृति के साथ प्राकृतिक और सामाजिक-दोनों प्रकार के बन्धनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मनुष्य की ऐतिहासिक प्रकृति का निर्धारण करने वाली शक्तियों की द्वैधता की धारणा को मार्क्स सिरे से खारिज करते हैं। सेक्सुअल शक्तियों और उत्पादक शक्तियों को वे एक-दूसरे के समकक्ष या समतुल्य नहीं मानते। प्रजनन या मानव जाति का पुनरुत्पादन ऐतिहासिक अस्तित्व की बुनियादी शर्त है लेकिन इतिहास मात्र मनुष्य का उद्भव और क्रम-विकास नहीं है। इतिहास की उत्पत्ति और विकास की कारक शक्ति उत्पादक शक्तियों के उपयोग, निर्माण और विकास में निहित है जो आम तौर पर मानव-सम्बन्धों को, और साथ ही, खास तौर पर, सेक्सुअल सम्बन्धों की मानवीय अन्तर्वस्तु और रूप को भी निर्धारित करते हैं। मानवीय स्वत्व शुरू से ही केवल प्राकृतिक नहीं, बल्कि सर्वोपरि तौर पर ऐतिहासिक रहा है। स्त्री और पुरुष के बीच के रिश्तों का विकास (उनके बीच प्रेम की अवधारणा का विकास, यौन क्रिया का पाशवेतर, मानवीय कलात्मक विकास और परिवार संस्था का विकास) उत्पादक शक्तियों और उत्पादन-सम्बन्धों के विकास द्वारा ही निर्धारित और अनुकूलित होता है।
आदिम युगों के दौरान, जब मनुष्य अभी अपनी यात्रा में प्रकृति और पशुजगत से बहुत दूर नहीं निकल आया था, जब अभी निजी सम्पत्ति और उस पर आधारित असमानतापूर्ण सामाजिक सम्बन्धों का जन्म नहीं हुआ था, तब स्त्री-पुरुष के बीच के रिश्ते काफ़ी हद तक पाशविक जैविक आकर्षण और प्रजनन के दायरे में सीमित थे और उनमें शोषण या उत्पीड़न का कोई पहलू था ही नहीं। यानी जब सामाजिक श्रम-विभाजन का अस्तित्व नहीं था तब स्त्री-पुरुष के बीच एक ही श्रम-विभाजन था और वह था सेक्सुअल क्रिया में श्रम-विभाजन (मार्क्स-एंगेल्स: जर्मन आइडियोलॉजी, पूर्वोद्धृत, पृ- 42–43)। इसमें विपरीत तत्वों के संघात और एकता के रूप में अन्तर्क्रिया का द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त तो काम करता था, लेकिन दोनों में से किसी एक की भूमिका उत्पीड़क की और दूसरे की उत्पीड़ित की नहीं थी। सामाजिक श्रम-विभाजन और उसमें निहित सभी अन्तरविरोधों के विकास के साथ ही स्त्री-पुरुष के रिश्तों में भी परिवर्तन आया। यौन क्रिया और उससे जुड़े मनोभावों के सन्दर्भ में भी एक की स्थिति उत्पीड़क की और दूसरे की उत्पीड़ित की हो गयी। यह सामाजिक श्रम-विभाजन परिवार में श्रम के प्राकृतिक विभाजन और समाज के परस्पर–विरोधी पारिवारिक इकाइयों में विलगाव पर आधारित था जो साथ-साथ श्रम और उसके उत्पाद के, और इस रूप में सम्पत्ति के, परिमाणात्मक और गुणात्मक, असमान बँटवारे को जन्म देता था। परिवार में स्त्रियों और बच्चों की पुरुषों के बरक्स गुलाम जैसी स्थिति बन गयी। परिवार में यह गुलामी बेहद भोंड़े रूप में थी, लेकिन यही प्रच्छन्न गुलामी सम्पत्ति का पहले रूप का आधार थी। (विस्तार के लिए, मार्क्स और एंगेल्स: 'जर्मन आइडियोलॉजी', पूर्वोद्धत, पृ- 44)।
निजी सम्पत्ति के अग्रगामी विकास ने ही पारिवारिक जीवन और स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के रूपों के विकास का निर्धारण किया। निजी सम्पत्ति और श्रम-विभाजन ने परिवार को समुदाय के भीतर अलग-थलग कर दिया और इसे सामुदायिक यथार्थ के बजाय एक निजी यथार्थ बना दिया। एक पृथक्कृत घरेलू अर्थव्यवस्था का निर्धारण सीधे-सीधे निजी सम्पत्ति की गति ही करती है। यदि हम समकालीन बुर्जुआ समाज को भी देखें तो नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) और राज्य की मान्यता प्राप्त और पूर्वगृहीत आधारशिला इसमें भी परिवार ही है। चूँकि निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध ही वे बन्धन हैं जो आभासी या भ्रामक समुदाय और इसके सदस्यों को वस्तुओं के प्राकृतिक जगत से बाँधने का काम करते हैं, या यूँ कहें कि उन्हें इसके साथ परकीयकृत रूप में (इन एलियनेशन) जोड़ते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि विवाह "निश्चित तौर पर विशिष्ट निजी सम्पत्ति का एक रूप है" (मार्क्स: मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844, पृ- 133, इण्टरनेशनल पब्लिशर्स, न्यूयार्क, 1964)।
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति'में फ्रेडरिक एंगेल्स ने इतिहास और नृतत्वशास्त्र की खोजों के आधार पर यह दर्शाया है कि मानव-विकास के तीन मुख्य युगों के अनुरूप विवाह के तीन मुख्य रूप मिलते हैं: जंगल युग में यूथ विवाह, बर्बर युग में युग्म विवाह और सभ्यता के युग में एकनिष्ठ विवाह और उसके साथ जुड़ा हुआ व्यभिचार और वेश्यावृत्ति। बर्बर युग की उन्नत अवस्था में, युग्म परिवार तथा एकनिष्ठ विवाह के दौर में, दासियों पर पुरुषों का आधिपत्य और बहुपत्नी-प्रथा आम बात थी। नृतत्वशास्त्र और इतिहास की अधुनातन खोजें भी इसी बात को सिद्ध करती हैं कि अन्य संस्थाओं की ही भाँति मानव-विकास के साथ-साथ परिवार के स्वरूप में भी बदलाव आया और इसकी प्रमुख मंजिलें उत्पादक शक्तियों के विकास और मनुष्यों के बीच के सम्बन्धों में आये गुणात्मक परिवर्तनों से निर्धारित हुईं। आदिम मनुष्यों के समय से सभ्य जगत तक की यात्रा के दौरान परिवार के स्वरूप में आये आधारभूत बदलाव के बारे में एंगेल्स की प्रमुख स्थापना यह है कि एकनिष्ठ परिवार की अन्तिम विजय सभ्यता की शुरुआत का एक लक्षण था और कि यह एकनिष्ठ परिवार पुरुष-श्रेष्ठता पर आधारित था जिसमें पिता की सम्पित्त के उत्तराधिकार के लिए निर्विवाद पितृत्व वाली सन्तान पैदा करना स्त्री के लिए ज़रूरी था। प्राचीन ग्रीक समाज के अध्ययन के आधार पर एंगेल्स ने दर्शाया कि स्त्री-पुरुष के बीच एकनिष्ठ सम्बन्ध वैयक्तिक यौन–प्रेम (सेक्स-लव) या स्त्री-पुरुष के बीच बराबरी के रिश्ते के रूप में नहीं बल्कि स्त्री की पुरुष-अधीनस्थता के रूप में, इतिहास के प्रथम वर्ग-विभाजन और वर्ग-शोषण एवं वर्ग-उत्पीड़न के उत्पन्न होने के साथ-साथ, स्थापित हुआ। एकनिष्ठ स्त्री-पुरुष सम्बन्ध (मोनोगैमी) तब पैदा हुआ जब एक पुरुष के हाथों में पर्याप्त सम्पत्ति संकेन्द्रित हो गयी और यह चाहत पैदा हुई कि वह सम्पत्ति किसी दूसरे के बच्चों को न मिले। पर इसके लिए केवल स्त्री की एकनिष्ठता ही ज़रूरी थी। और ऐसा ही हुआ। शुरू से लेकर आज तक एकनिष्ठ सम्बन्ध केवल स्त्री के लिए अनिवार्य रहे हैं। पुरुष की यौन–स्वतंत्रता आद्यन्त अक्षत रही है। विवाहेतर सम्बन्ध या कई पुरुषों से यौन-सम्बन्ध स्त्रियों के लिए तो भयंकर सामाजिक-क़ानूनी सज़ा का हक़दार बनाने वाला अपराध रहा है, लेकिन पुरुष के लिए वह या तो सम्माननीय या सामाजिक मान्यताप्राप्त या ज्यादा से ज्यादा, एक मामूली, सहनीय नैतिक धब्बा रहा है। एंगेल्स लिखते हैं: "पुराने परम्परागत हैटेरिज्म को माल का वर्तमान पूँजीवादी उत्पादन जितना ही बदलता और अपने रंग में ढालता जाता है, उतना ही समाज पर उसका अधिक खराब असर पड़ता है। स्त्रियों में वेश्यावृत्ति केवल उन्हीं अभागिनों को पतन के गड्ढे में ढकेलती हैं जो उसके चंगुल में फ़ँस जाती हैं, और इन स्त्रियों का भी उतना पतन नहीं होता जितना आम तौर पर समझा जाता है। परन्तु दूसरी ओर, वेश्यावृत्ति सारे पुरुष संसार के चरित्र को बिगाड़ देती है और इस प्रकार दस में से नौ उदाहरणों में विवाह के पहले सगाई की लम्बी अवधि कार्यतः दाम्पत्य (से) बेवफ़ाई की ट्रेनिंग की अवधि बन जाती है।" (एंगेल्स: परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति', मार्क्स-एंगेल्स: संकलित रचनाएँ, खण्ड-3, भाग-2, पृ- 88, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1978)।
अब सवाल यह उठता है कि यदि परिवार की उत्पत्ति और सभ्य जगत में उसके आधार के बारे में ये बातें सही हैं, तो समाजवादी संक्रमण के अन्तर्गत, जब उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व का उन्मूलन हो जायेगा और कम्युनिज्म के अन्तर्गत, जब वर्ग-सम्बन्धों का ही विलोपन हो जायेगा, तो उन स्थितियों का परिवार या विवाह संस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके उत्तर के लिए और भावी समाज में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध के आम स्वरूप को जानने के लिए हमें एंगेल्स को फ़िर किंचित विस्तार से उद्धृत करना पड़ेगा: "अब हम एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप एकनिष्ठ विवाह का वर्तमान आर्थिक आधार उतने ही निश्चित रूप से मिट जायेगा, जितने निश्चित रूप से एकनिष्ठ विवाह के अनुपूरक का, वेश्यावृत्ति का आर्थिक आधार मिट जायेगा। …-आने वाली सामाजिक क्रान्ति स्थायी दायाद्य (हेरिटेबल) धन-सम्पदा के अधिकतर भाग को-यानी उत्पादन के साधनों को-सामाजिक सम्पत्ति बना देगी और ऐसा करके सम्पत्ति की विरासत के बारे में इस सारी चिन्ता को अल्पतम कर देगी। पर एकनिष्ठ विवाह चूँकि आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, इसलिए क्या इन कारणों के मिट जाने के बाद वह भी मिट जायेगा?
"इस प्रश्न का यह उत्तर शायद ग़लत नहीं होगा: मिटना तो दूर, एकनिष्ठ विवाह तब जाकर ही पूर्णता प्राप्त करने की ओर बढ़ेगा। कारण कि उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व में रूपान्तरण के फ़लस्वरूप उजरती श्रम, सर्वहारा वर्ग भी मिट जायेगा और उसके साथ-साथ यह आवश्यकता भी जाती रहेगी कि एक निश्चित संख्या में-जिस संख्या को हिसाब लगाकर बताया जा सकता है-स्त्रियाँ पैसे लेकर अपनी देह को पुरुषों के हाथों में सौंप दें। तब वेश्यावृत्ति का अन्त हो जायेगा और एकनिष्ठ विवाह-प्रथा मिटने के बजाय, पहली बार पुरुषों के लिए भी वास्तविकता बन जायेगी।" (एंगेल्स: पूर्वोद्धृत, पृ- 88–89)।
लेकिन फ़िर एंगेल्स यह सवाल उठाते हैं कि जब उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व हो जाने के बाद वैयक्तिक परिवार समाज की आर्थिक इकाई नहीं रह जायेगा, जब घर का निजी प्रबन्ध, बच्चों का लालन–पालन और शिक्षा एक सार्वजनिक मामला हो जायेगा, जब किसी लड़की को मनचाहे पुरुष को प्यार करने से रोकने वाले आर्थिक, सामाजिक और नैतिक कारणों का भौतिक आधार ही समाप्त हो जायेगा, तब क्या वेश्यावृत्ति के साथ-साथ एकनिष्ठ विवाह भी (क्योंकि ये दोनों विपरीत होते हुए भी एक ही सामाजिक व्यवस्था के दो सिरे हैं) समाप्त नहीं हो जायेगा और तब क्या पूर्णतः अनियंत्रित, स्वच्छन्द यौन-सम्बन्धों का घटाटोप नहीं छा जायेगा? एंगेल्स इस भ्रान्ति को सिरे से खारिज करते हुए इतिहास में आविर्भूत उस नये तत्व की महत्ता को रेखांकित करते हैं जिसे व्यक्तिगत यौन–प्रेम या सामान्य तौर पर रोमानी (रोमैण्टिक) प्यार कहा जाता है। यह सभ्यता का युग शुरू होते समय, यानी एकनिष्ठ विवाह के विकसित होने के समय ज्यादा से ज्यादा केवल बीज रूप में ही मौजूद था। इसका वास्तविक अर्थों में विकास पूँजीवाद के आगमन के बाद ही हुआ। तमाम आर्थिक-सामाजिक बाध्यताओं की समाप्ति के बाद, पूरी तरह से पारस्परिक आकर्षण, भावनात्मक (और भावना विचारों से विच्छिन्न कोई चीज़ नहीं होती) एकता, समानता और स्वतंत्र चाहत पर आधारित व्यक्तिगत यौन–प्रेम या रोमानी प्रेम ही स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का आधार होगा। यह व्यक्तिगत यौन–प्रेम चूँकि प्रकृति से ही एकान्तिक होता है, इसलिए पूँजीवाद की समाप्ति के बाद ही सच्चे अर्थों में एकनिष्ठ स्त्री-पुरुष सम्बन्ध स्थापित हो सकेंगे, या कहें कि केवल तभी जाकर, स्त्री-पुरुष दोनों के लिए, सच्चे अर्थों में प्रेम करने की आज़ादी कायम हो सकेगी। आज के प्रेम-सम्बन्ध या एकनिष्ठ विवाह में जो एकान्तिकता होती है, वह पूर्ण रूप में केवल स्त्री के लिए ही होती है, जबकि पुरुष इससे स्वतंत्र होता है।
इस बात को भली-भाँति समझने के लिए थोड़ा और विस्तार में जाने की ज़रूरत है। आधुनिक काल का यौन प्रेम या रोमानी प्रेम या 'पैशन लव'प्राचीन काल की सरल यौनेच्छा या 'ईरोस' (eros) से बहुत अलग चीज़ है। प्राचीनकालीन 'ईरोस'में औरत की चाहत का कोई विशेष महत्व नहीं होता था, जबकि यौन–प्रेम दोतरफ़ा होता है, यानी यह मानकर चलता है कि प्रेम करने पर प्रेम मिलता भी है। यह एक उत्कट भाव होता है जिसमें प्रेमी-प्रेमिका को लगता है कि वे एक-दूसरे के बिना जी नहीं सकते। इसमें सम्भोग को केवल क़ानूनी नहीं बल्कि नैतिक मानकों से देखा जाता है और पारस्परिक प्रेम का परिणाम होने पर ही उसे स्वीकार्य माना जाता है। प्राचीन काल में प्रेम की उत्कटता या तो स्वतंत्र नागरिकों के अधिकृत समाज से बाहर दासों के बीच देखने को मिलती थी या फ़िर विवाहेतर यौन–व्यापार में, और वह भी अधिकृत समाज से बाहर समझी जाने वाली स्त्रियों-यानी हैटेराओं के साथ प्रेम में देखने को मिलती थी। यानी प्राचीन समाज के स्वतंत्र नागरिकों में यदि सचमुच प्रेम होता भी था तो केवल विवाह के बन्धन तोड़कर, व्यभिचार के रूप में। पति-पत्नी के बीच जो थोड़ा-बहुत प्रेम देखने में आता भी था, तो वह मनोगत प्रवृत्ति नहीं बल्कि वस्तुगत कर्त्तव्य था। वह विवाह का कारण नहीं बल्कि उसका पूरक था। विवाह माता-पिता की मर्जी और बड़े-बुजुर्गों की स्वीकृति से ही होते थे। व्यक्तिगत सौन्दर्य, अन्तरंग साहचर्य, समान रुचि आदि से उस समय भी स्त्री-पुरुष में परस्पर सम्भोग की इच्छा उत्पन्न होती थी, पर उनके लिए इस बात का कोई मतलब नहीं होता था कि वे किसके साथ यह अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं।
मध्ययुग में भी स्त्री-पुरुष के बीच प्रेम और विवाह के बारे में यही स्थिति बनी रही। सामन्ती उत्पादन-सम्बन्ध के अनुरूप विवाह एक ऐसा सामाजिक सम्बन्ध था जिसमें लड़की केवल भोग्या ही हो सकती थी और विवाह-सूत्र में बँधने वाले जोड़े के स्वतंत्र निर्णय का कोई मतलब नहीं था। पुरुष के लिए पत्नी वंश चलाने का निमित्त-मात्र थी और काम-तृप्ति के लिए वह बिना किसी प्रेम के दासी या वेश्या के पास जा सकता था। मध्यकाल में यदि आज के यौन–प्रेम का प्रारम्भिक रूप कहीं दीखता भी है तो वह विवाह-सम्बन्ध के विरुद्ध विद्रोह के रूप में, नाइटों के परकीया प्रेम-सम्बन्धों या विवाहेतर प्रेम-व्यापार में दीखता है। आम तौर पर तब विवाह नाइट या सामन्त और राजा या राजकुमार के लिए एक राजनीतिक मामला होता था जिसमें निजी इच्छा या आकांक्षा के बजाय सामन्तकुल या राजकुल के हित निर्णायक हुआ करते थे। यही बात मध्ययुग के नागरिकों के लिए भी लागू होती थी। शिल्प-संघों के अधिकार-पत्र और विशेष शर्तें किसी नागरिक को दूसरे शिल्प-संघों से, अपने ही संघ के दूसरे सदस्यों से और अपने मज़दूर कारीगरों और शार्गिदों से क़ानूनी तौर पर अलग रखने तथा उसके विशेषाधिकारों की हिफ़ाजत के लिए जो बनावटी सीमाएँ बनाती थीं, उसी संकीर्ण दायरे के भीतर ही उस नागरिक का विवाह होता था और वह भी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं बल्कि पारिवारिक हित से तय होता था।
प्रेम और विवाह के ये रूप विश्व इतिहास के रंगमंच पर पूँजीवाद के विजय-अभियान के प्रारम्भ तक बने रहे। विवाह का प्राचीन और मध्यकालीन रूप पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के लिए भी सर्वथा उपयुक्त था, लेकिन विडम्बना यह थी कि सामन्ती विशेषाधिकारों, पुराने परम्परागत सम्बन्धों, रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक अधिकारों की जगह क्रय-विक्रय और "स्वतंत्र"क़रार को स्थापित किये बिना कच्चे माल, श्रम शक्ति और वर्कशापों के उत्पाद सहित हर चीज़ को बिकाऊ माल बनाना सम्भव ही नहीं था। और यह "स्वतंत्र"क़रार "स्वतंत्र"और "समान"लोगों के बीच ही सम्भव था। पूँजीवादी जनवादी क्रान्तियों की वैचारिक-सांस्कृतिक पूर्वपीठिका तैयार करते हुए यूरोप के पुनर्जागरणकालीन महामानवों ने, लूथर और काल्बैं के धर्म-सुधार आन्दोलन ने और प्रबोधनकालीन दार्शनिकों ने मध्ययुगीन निरंकुशता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जनमानस को तैयार करते हुए जो काम किया, वह एक महान प्रगतिशील ऐतिहासिक काम था, पर वस्तुगत तौर पर वह बुर्जुआ वर्ग के हितों की ही विचारधारात्मक अभिव्यक्ति था। धर्म-सुधार आन्दोलन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर व्यक्ति केवल तभी अपने कार्यों के लिए पूर्णतः ज़िम्मेदार माना जायेगा जब वह पूरी आज़ादी के साथ काम करे; और हर आदमी का नैतिक कर्त्तव्य है कि वह अनैतिक कार्य करने के हर दबाव का विरोध करे। पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के लिए ज़रूरी"स्वतंत्र"व्यक्तियों के बीच "स्वतंत्र"क़रार की स्थिति बनाने में यह नैतिक-सामाजिक नियम सहायक था, पर एक आम नियम के तौर पर इसका चलन में आना जाहिरा तौर पर विवाह की पुरानी संस्था पर भी चोट पहुँचाने वाला था। ठीक इसी प्रकार पुनर्जागरणकाल के महानायकों ने मानवतावाद के सिद्धान्त-प्रतिपादन द्वारा जब सामन्ती विशेषाधिकारों की अलौकिक स्वीकृति पर चोट की तो यह विवाह की अलौकिक स्वीकृति पर भी एक चोट बन गयी। विवाह के पीछे नियति नहीं, बल्कि "स्वतंत्र"मनुष्यों की "स्वतंत्र"पारस्परिक सहमति होती है, इस तर्क की स्वीकार्यता के बाद आधुनिक युग के यौन–प्रेम के मनोभाव का जन्म होना ही था। इस तरह, हालाँकि पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली का मध्ययुगीन विवाह-प्रथा से कोई बैर–भाव नहीं था, लेकिन पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली की स्थापना के लिए बुर्जुआ वर्ग की राजनीतिक विजय तथा उसके लिए बुर्जुआ मानवतावादी एवं जनवादी विचारों का जनमानस पर प्रभावी होना ज़रूरी था और इस प्रक्रिया की अनिवार्य तार्किक परिणति थी, तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ ही मध्यकालीन विवाह और परिवार संस्था में आमूल परिवर्तन। पुनर्जागरणकाल के दार्शनिक जब इस काम को कर रहे थे तो वे बुर्जुआ वर्ग और पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के सचेतन हित-साधन का काम नहीं कर रहे थे। उनके महान आदर्श पहले से ही व्यवस्थित हो चुके बुर्जुआ समाज की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि "आम क्रान्ति के बीच"विकसित हुए थे। यह उनकी इच्छा से स्वतंत्र था कि उन आदर्शों का मूर्त रूप बुर्जुआ सामाजिक ढाँचे के रूप में ही सामने आना था। उन्हें मानवता को कुछ मध्ययुगीन बुराइयों से छुटकारा दिलाना था और कुछ ऐसे आदर्शों की अनश्वर मशाल जलानी थी, जिन्हें पूँजीवादी व्यवस्था के अन्त तक मानव जाति अपना प्रेरणा-स्रोत मानकर चलेगी। पुनर्जागरण-काल के दौरान सामाजिक सम्बन्ध अविराम रूप से गतिशील और परिवर्तनशील थे और अभी वे व्यक्तिगत पहल, प्रतिभा और योग्यताओं के विकास को काफ़ी हद तक रोकने वाली ऐसी शक्ति नहीं बने थे, जैसा कि वे बुर्जुआ समाज में बने। इसी के चलते पुनर्जागरण के नायकों के बारे में एंगेल्स ने लिखा है: "बुर्जुआ वर्ग के आधुनिक शासन के संस्थापक स्वयं बुर्जुआ परिसीमाओं से सर्वथा मुक्त थे"और यह भी कि, "उस युग के नायक अभी तक श्रम-विभाजन की दासता से बँधे नहीं थे, जिसके एकांगीपन पैदा करने वाले, संकुचनकारी प्रभाव हम उनके उत्तरवर्तियों में पाते हैं" (फ्रेडरिक एंगेल्स: 'डायलेक्टिक्स ऑफ़ नेचर', पृ- 2–3, इण्टरनेशनल पब्लिशर्स, न्यूयार्क, 1963)। यही वह विशिष्टता थी जिसके चलते पुनर्जागरणकाल के मानवतावाद, व्यक्तिवाद और लौकिकतावाद के युगान्तरकारी विचारों ने जनजीवन पर उतना गहरा प्रभाव छोड़ा, जितना पहले शायद कभी किसी क्रान्ति द्वारा प्रसूत विचारों ने नहीं छोड़ा था। इन विचारों ने पहली बार स्त्री को सम्भोगनीय और शिशुप्रसवा जीव से इतर, भावनाओं से युक्त स्वतंत्र अस्मिता वाली नागरिक मानने का आधार तैयार किया और आधुनिक यौन–प्रेम, रोमानी प्रेम या भावावेगी प्रेम (पैशल लव) की अवधारणा पैदा हुई। सौन्दर्य, काम-भावना (पाशविक आवेग से भिन्न सौन्दर्याकर्षण और साहचर्य-प्रेरित ऐन्द्रिक आकर्षण), ऐन्द्रिकता आदि की नयी अवधारणाएँ भी इसी आधार पर पैदा हुईं। इनके ऐतिहासिक साक्ष्य हम पुनर्जागरणकालीन चित्रकला, महाकाव्यों और नाटकों में आसानी से पा सकते हैं।
महान फ्रांसीसी बुर्जुआ जनवादी क्रान्ति की पूर्वपीठिका तैयार करने वाले प्रबोधनकाल (एज ऑफ़ एनलाइटेनमेण्ट) दार्शनिकों के बारे में भी काफ़ी हद तक वही बातें कही जा सकती हैं, जो पुनर्जागरण के नायकों की क्रान्तिकारी विशिष्टता और उसके वस्तुगत कारणों के बारे में ऊपर कही गयी हैं। प्रबोधन सामाजिक-राजनीतिक-दार्शनिक-कलात्मक चिन्तन के क्षेत्र में एक आन्दोलन–मात्र नहीं था बल्कि फ्रांसीसी क्रान्ति की पूर्वबेला में सामन्तवाद-निरंकुशतावाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए उठ खड़े हो रहे, अग्रगामी बुर्जुआ वर्ग के हितों की विचारधारात्मक अभिव्यक्ति था। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के जनवादी आदर्शों और तर्कणा को निर्णय की कसौटी बनाने के विचार ने व्यापक जनमानस को प्रभावित किया तो स्त्री-पुरुष सम्बन्धों पर और स्त्री अधिकारों पर भी लाजिमी तौर पर इसका प्रभाव पड़ना ही था। पहली बार प्रेम के अधिकार को और विवाह के मामले में जोड़े के स्वतंत्र निर्णय के अधिकार को इस हद तक सामाजिक मान्यता मिली कि चर्च को भी इसे अनिच्छापूर्वक स्वीकार करना पड़ा।
लेकिन बुर्जुआ वर्ग की विजय के बाद, इन सभी आदर्शों का एक प्रहसनात्मक व्यंग्य-चित्र सामने आया। समय ने सिद्ध किया कि प्रबोधनकालीन विचार बुर्जुआ जीवन के यथार्थ के एक आदर्शीकृत अमूर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं थे। स्वतंत्रता का व्यावहारिक रूप शोषण की स्वतंत्रता और श्रमशक्ति बेचने की स्वतंत्रता के रूप में तथा छोटे मालिकों और किसानों की सम्पत्ति से"स्वतंत्रता"के रूप में सामने आया। शाश्वत न्याय ने बुर्जुआ न्याय में मूर्त रूप धारण किया। समानता क़ानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति की बुर्जुआ समानता में परिणत हो गयी। बुर्जुआ सम्पत्ति को मनुष्य का मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। एंगेल्स के शब्दों में, "जब फ्रांसीसी क्रान्ति ने इस तर्कबुद्धिसंगत समाज तथा इस तर्कबुद्धिसंगत राज्य को मूर्त रूप दिया, तो नयी संस्थाएँ पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं की तुलना में अपनी सारी तर्कबुद्धिसंगतता के बावजूद पूर्ण तर्कबुद्धिसंगत कदापि नहीं सिद्ध हुई।"लोभ और लाभ की बुनियाद पर कायम इस नये समाज में, स्त्रियों की स्थिति में आये बदलाव उसे पूर्ण स्वतंत्र नागरिक कत्तई नहीं बना पाये। वह निकृष्टतम कोटि की उजरती गुलाम और दोयम दर्जे की नागरिक बन गयी। घरेलू गुलामी के बन्धन रूप बदलकर बने रहे। ऐसे में व्यक्तिगत और यौन–प्रेम का प्रबोधनकालीन आदर्श मूर्त हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वह स्त्रियों की समान सामाजिक हैसियत और निर्णय लेने की वास्तविक स्वतंत्रता के बिना सम्भव नहीं था। फ्रेडरिक एंगेल्स लिखते हैं: "पहले सामन्ती दुराचार दिन–दहाड़े होता था, अब वह एकदम समाप्त तो नहीं हो गया था, पर कम से कम पृष्ठभूमि में ज़रूर चला गया था। उसके स्थान पर बुर्जुआ अनाचार, जो इसके पहले पर्दे के पीछे हुआ करता था, अब प्रचुर रूप में बढ़ने लगा था। व्यापार अधिकाधिक धोखाधड़ी बनता गया। क्रान्तिकारी आदर्श-सूत्र के "बंधुत्व"ने होड़ के संघर्ष की ठगी तथा प्रतिस्पर्धा में मूर्त रूप प्राप्त किया। बल तथा उत्पीड़न का स्थान भ्रष्टाचार ने ले लिया। सामाजिक सत्ता का उत्तोलक तलवार के स्थान पर सोना बन गया। नववधु के साथ पहली रात सोने का अधिकार सामन्ती प्रभुओं से पूँजीवादी कारख़ानेदारों के पास पहुँच गया। वेश्यावृत्ति में इतनी अधिक वृद्धि हो गयी, जो पहले कभी सुनी तक नहीं गयी थी। स्वयं विवाह-प्रथा पहले की तरह अब भी वेश्यावृत्ति का क़ानूनी मान्यता प्राप्त रूप तथा उसकी सरकारी आड़ बनी हुई थी, और इसके अलावा व्यापक परस्त्रीगमन उसके अनुपूरक का काम कर रहा था।" (एंगेल्स: 'ड्यूहरिंग मत-खण्डन', मार्क्स-एंगेल्स: 'साहित्य और कला'में उद्धृत, पृ- 316–17, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 1981)
पूँजीवादी विचारों के अनुसार, विवाह भी अन्य क़ानूनी क़रारों जैसा एक क़रार है और इस मायने में सबसे महत्वपूर्ण क़रार है कि उसके लिए दो व्यक्तियों के तन और मन का जीवन भर के लिए (जब तक क़रार की शर्त न टूटे) फ़ैसला कर दिया जाता है। अतः सभी क़रारों की तरह, इसमें भी दो युवा व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने आप का, अपने शरीरों का उपयोग करने का निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। यह वह युग था, जब पूरी दुनिया के बाज़ार पर कब्जा करने और पूँजी-संचय की आकांक्षा देशों की चौहद्दियों के अतिक्रमण के साथ ही सभी पुराने सामाजिक बन्धनों और परम्परागत विचारों को ध्वस्त कर रही थी। इसी क्रान्तिकारी युग में व्यक्तिगत यौन–प्रेम की नयी क्रान्तिकारी अवधारणा का विकास हुआ जो माल-उत्पादन की प्रणाली के स्थापित होने के बाद, सामाजिक जीवन में मूर्त रूप तो नहीं ले पायी, पर व्यक्तिगत यौन–प्रेम की यह भावना और आकांक्षा अपने आप में एक यथार्थ बन चुकी थी जिसने वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तकों को यह दिशा दी कि माल-उत्पादन की प्रणाली को समाप्त करके, स्त्री-पुरुष के बीच सच्चे एकनिष्ठ यौन–प्रेम को, इसकी राह में आड़े आने वाली आर्थिक बाध्यताओं और उन बाध्यताओं को सर्वाधिक मूर्त रूप में अभिव्यक्त करने वाली बुर्जुआ पारिवारिक संरचना को नष्ट करके, मानव-समाज की एक आम सच्चाई बनाया जा सकता है। पूँजीवाद ने कम से कम प्रेम विवाह के अधिकार (और प्रेम टूटने पर अलग होने के अधिकार) को मान्यता देने का एक प्रगतिशील काम किया; जिसे एक वास्तविकता बनाने का काम निजी सम्पत्ति पर आधारित सामाजिक सम्बन्धों को समाप्त करने वाली अग्रवर्ती सामाजिक क्रान्ति का एजेण्डा बन गया। इस मायने में मार्क्सवाद ने पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति के स्थगित एजेण्डे को ही आगे बढ़ाया और स्पष्ट किया कि पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों के उन्मूलन के साथ ही विवाह के पीछे पारस्परिक आकर्षण के अतिरिक्त कोई और कारण नहीं रह जायेगा और चूँकि यौन–प्रेम अपनी प्रकृति से ही एकान्तिक होता है, इसलिए उस स्थिति में यौन–प्रेम पर आधारित विवाह सच्चे मायने में एकनिष्ठ हुआ करेंगे। मार्क्स और एंगेल्स ने विवाह संस्था की अठारहवीं शताब्दी के विचारकों-लेखकों और फ्रांसीसी क्रान्ति द्वारा प्रस्तुत आलोचना को ही आगे बढ़ाया तथा तर्कसंगत बनाकर तार्किक निष्पत्ति तक पहुँचाया। उन्होंने स्वीकार किया है कि इन विचारकों ने और फ्रांसीसी क्रान्ति ने विवाह संस्था की बुनियाद को हिला दिया था (मार्क्स-एंगेल्स: 'जर्मन आइडियोलॉजी, पूर्वोद्धृत, पृ- 192–193)। उनके विचार से, पूँजीवाद-विरोधी क्रान्ति का मूल लक्ष्य उन तमाम जंजीरों को तोड़ डालना है जो मनुष्य के मानवीय होने की राह में बाधा हैं। प्यार अपनी सार्वभौमिकता में प्यार के रूप में अभिव्यक्त हो, उसके लिए बुर्जुआ विवाह और बुर्जुआ परिवार के उन्मूलन को वे ज़रूरी मानते हैं। केवल तभी मनुष्य के प्राकृतिक और सामाजिक सारतत्व का 'आब्जेक्टिफ़िकेशन'हो सकेगा।
एक बुर्जुआ सामाजिक-आर्थिक संरचना के भीतर यह सम्भव ही नहीं है, इस बात को अहसास के और अधिक गहरे धरातल पर जाकर समझने के लिए सामाजिक श्रम विभाजन से पैदा होने वाले परकीयरकण या अलगाव (एलियनेशन) की मार्क्सवादी अवधारणा पर भी थोड़ी चर्चा ज़रूरी है।
मार्क्सीय अवधारणा के रूप में परकीयकरण या अलगाव एक ऐसी क्रिया (और साथ ही अवस्था) है जिसमें मनुष्य (एक व्यक्ति, समूह, संस्था या समाज) (1) अपने स्वयं कार्यकलाप के परिणाम या श्रम के उत्पाद से (और स्वयं अपने कार्यकलाप या श्रम से), (2) उस प्रकृति से, जिसमें वह रहता है, (3) दूसरे मनुष्यों से और इन सबके परिणामस्वरूप (4) स्वयं अपने आप से (ऐतिहासिक रूप से सृजित अपनी खुद की मानवीय सम्भावनाओं और मानवीय सारतत्व से) से बेगाना हो जाता है। यानी परकीयकरण या अलगाव मनुष्य के व्यावहारिक कार्यकलाप की उपज (श्रम की उपज, मुद्रा, सामाजिक सम्बन्ध आदि) और सैद्धान्तिक भावनात्मक कार्यकलाप की उपज-इन दोनों को, और साथ ही मनुष्य के गुणों और क्षमताओं को, ऐसी चीज़ों में बदल देने की प्रक्रिया और परिणाम है, जो लोगों से स्वतंत्र हो और जिसका उनपर प्रभुत्व हो। दूसरे, यह घटनाओं, प्रक्रियाओं और सम्बन्धों का उनके निज रूप से भिन्न किसी वस्तु में रूपान्तरण है तथा, जीवन में लोगों के वास्तविक सम्बन्धों का, उनकी चेतना में विकृतिकरण है। आगे चलकर, कुछ मार्क्सवादी विद्वानों ने अलगाव के विभिन्न रूपों का प्रवर्गीकरण करने की भी कोशिश की। जैसे, एडम शैफ़(Adam Schaff) ने इसके दो बुनियादी रूपों की बात की है: वस्तुगत अलगाव (या सामान्य अलगाव) और मनोगत अलगाव। शाक्तेल (Schachtel) ने इसकी चार श्रेणियाँ बनाई हैं: मनुष्यों का प्रकृति से अलगाव, अपने साथ के मनुष्यों से अलगाव, अपने हाथों और दिमाग़ के कामों से अलगाव और स्वयं से अलगाव। सीमैन ने इसकी पाँच श्रेणियाँ निर्धारित की है: अधिकारहीनता, सार्थकताहीनता, सामाजिक पार्थक्य, प्रतिमानहीनता (नॉर्मलेसनेस) और आत्मविच्छिन्नता (सेल्फ़-एस्ट्रेंजमेण्ट) (देखिए: 'ए डिक्शनरी ऑफ़ मार्क्सिस्ट थॉट,'पृ- 15, माया ब्लैकवेल वर्ल्डन्यू रेफ़रेंस, इण्डियन रीप्रिण्ट, नई दिल्ली, 2000)। ये सख़्त या जड़ीभूत प्रवर्गीकरण इन अर्थों में ठीक नहीं है क्योंकि ये एक ही सामाजिक परिघटना के विविध वस्तुगत और मनोगत आयाम या पहलू हैं।
मार्क्स के विचार से अलगाव समाज-विकास की एक निश्चित मंजिल के अन्तरविरोधों को व्यक्त करता है। वह श्रम-विभाजन से जन्मा और निजी स्वामित्व से जुड़ा हुआ है। ऐसी अवस्थाओं में सामाजिक सम्बन्ध स्वयंस्फ़ूर्त ढंग से बनते हैं और लोगों के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं जबकि कार्यकलाप के फ़लों और उपजों का व्यक्तियों और सामाजिक समूहों से अलगाव हो जाता है और वे या तो दूसरे लोगों द्वारा या किसी अलौकिक शक्ति द्वारा थोपी गयी वस्तु के रूप में प्रकट होते हैं। अलगाव-विषयक मार्क्स की अवधारणा उनके द्वारा "विच्छिन्न श्रम"या "वियोजित श्रम" (इस्ट्रेंज्ड लेबर) की विवेचना में स्पष्ट होकर सामने आती है। मार्क्स ने स्पष्ट किया कि श्रम की किसी वस्तु में समाविष्ट ऐसा श्रम, जो मूर्त हो गया है, श्रम का वस्तुकरण (आब्जेक्टिफ़िकेशन) है और निजी सम्पत्ति द्वारा शासित समाज में श्रम का वस्तुकरण अनिवार्यतः श्रमिक को जीवन के आनन्दों से वंचित करता है, उसे अपने श्रम के वस्तु का दास बना देता है। उसके श्रम का उत्पाद उसके लिए एक बेगाना उत्पाद बन जाता है और वस्तुकृत श्रम परकीयकृत या अलगाव-भूत (एलियनेटेड) श्रम बन जाता है। श्रम-प्रक्रिया अपनी सृजनात्मक अन्तर्वस्तु को खो देती है और श्रमिक के लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता। श्रमिक के पास इसके लिए कोई प्रेरणा नहीं होती कि वह सौन्दर्य के नियमों और सार्वजनिक आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करे। अपनी शारीरिक-मानसिक शक्ति के स्वेच्छया विकास से वंचित मात्र पशुवत् आदिम आवश्यकताओं के साथ जीता हुआ वह पशु-सदृश हो जाता है, मनुष्य के सन्निहित गुणों से रिक्त हो जाता है तथा अमूर्तन, स्वप्न और कल्पना की शक्ति को, प्यार की मानवीय सम्भावनाओं को खो देता है। वह स्वयं अपनी बेड़ियाँ बनाता है। वह अपना रह ही नहीं जाता बल्कि पूँजी के स्वामी का हो जाता है। यानी अलगाव मनुष्य को मनुष्य से और मानवीय गुणों-सम्भावनाओं से अलग कर देता है। इस रूप में हर अलगाव, अनिवार्यतः आत्मअलगाव भी होता है। (इस विस्तृत विवेचना के लिए देखें, मार्क्स: 'इकोनॉमिक एण्ड फ़िलॉसोफ़िक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844', फ़र्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट, 'इस्ट्रेज्ड लेबर', पृ- 66–80, नेशनल बुक एजेंसी, कलकत्ता, 1993)।
अलगाव के बुनियादी वस्तुगत कारणों की विवेचना, उसके रूपों के उद्घाटन और रैडिकल आलोचना का समाहार मार्क्स इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि रैडिकल क्रान्ति के द्वारा पूँजीवादी श्रम-विभाजन को और निजी सम्पत्ति को समाप्त करके ही मनुष्य के विघटित व्यक्तित्व को पुनस्संगठित किया जा सकता है, उसके आत्मनिर्वासन और आत्म-अलगाव की स्थिति का अतिक्रमण किया जा सकता है और स्वयं तक उसकी वापसी को, मनुष्य द्वारा मनुष्य के लिए मानव-प्रकृति की बहाली को सम्भव बनाया जा सकता है। पूँजीवादी सामाजिक श्रम-विभाजन को समाप्त करके ही वि-अलगाव या वि-परकीयकरण (डी–एलियनेशन) को सम्भव बनाया जा सकता है और व्यक्तिगत एकान्तिक यौन–प्रेम या रोमानी प्रेम या भावावेगी प्रेम (पैशन लव) का जो आदर्श प्रबोधन-काल के विचारकों और यूटोपियाई समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था, उसे एक यथार्थ में रूपान्तरित किया जा सकता है।
यहाँ पर एक भ्रान्ति का निवारण भी ज़रूरी है। मार्क्स जब मानव-प्रकृति या मानवीय सारतत्व की फ़िर से बहाली की और मनुष्य की मनुष्य तक वापसी की बात करते हैं तो उनका मतलब न तो मानव-प्रकृति या मानवीय सारतत्व को जड़ या अपरिवर्तनीय मानने से है, न ही अनैतिहासिक ढंग से वे यह मानते हैं कि ऐसी कोई अचल संकल्पना या चीज़ अतीत में यथार्थ रूप में मौजूद थी, फ़िर खो गयी और अब उसे फ़िर से हासिल करना है। अलगाव को मार्क्सवाद किसी तथ्यात्मक या आदर्श ('नॉर्मेटिव') मानव-प्रकृति से नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से सृजित मानवीय सम्भावनाओं से अलगाव के रूप में, विशेषकर स्वतंत्रता और सर्जनात्मकता की मानवीय क्षमता से अलगाव के रूप में देखता-समझता है। आत्म-अलगाव की अवधारणा मनुष्य की किसी जड़, अनैतिहासिक अवधारणा प्रस्तुत करने के बजाय मनुष्य के सतत्-पुनर्नवीकरण और विकास की प्रक्रिया को संवेग प्रदान करने का आह्वान करती है। जैसा कि मिलान कांग्रगा कहते हैं, आत्म-अलगाव का शिकार होने का मतलब है अपने कार्य से अलगाव, आत्म-सक्रियता से, आत्म-उत्पादन से, आत्म-सर्जना से अलगाव, मानव-व्यवहार और एक मानवीय उत्पाद के रूप में इतिहास से अलगाव ('एक डिक्शनरी ऑफ़ मार्विन्सस्ट थॉट'में उद्धृत, पूर्वोद्धृत, पृ- 14)। यानी एक मनुष्य के अलगावग्रस्त या आत्म-अलगावग्रस्त होने का मतलब है कि उसके सतत् मनुष्य होने की क्रिया रुक गयी है और बनी-बनायी दुनिया में जीते हुए वह व्यावहारिक-आलोचनात्मक ढंग से, क्रान्तिकारी ढंग से सक्रिय नहीं है। यानी जैसा कि ए.पी. ओगुर्त्सोव (सोवियत इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ फ़िलॉसाफ़ेी) कहते हैं, अलगाव एक दार्शनिक और समाजशास्त्रीय प्रवर्ग है जो मनुष्य के कार्यकलापों और उसके परिणामों के, ऐसी स्वतंत्र शक्तियों में वस्तुगत रूपान्तरण को अभिव्यक्त करता है, जो उस पर आधिपत्य कायम कर लेती हैं और उसके प्रतिकूल होती हैं। साथ ही, यह सामाजिक प्रक्रिया की एक सक्रिय मनोगत शक्ति से एक वस्तु में मनुष्य के रूपान्तरण की क्रिया को भी अभिव्यक्त करती है।
उपरोक्त भ्रान्ति का निवारण इसलिए ज़रूरी था कि हम इस बात को जान लें कि सवाल अतीत में मौजूद मानवीय प्यार या मूल्य के किसी प्रतिमान की पुनर्प्राप्ति का नहीं है। सवाल मनुष्य के प्राकृतिक जगत से क्रमशः दूर जाते हुए, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य होते जाने के उस गुण को फ़िर से हासिल करने का है जिसे वर्ग-समाज के विकास के दौरान, व्यक्तित्व के विघटन के साथ खोने की प्रक्रिया पूँजीवाद के वर्तमान वार्धक्य-काल तक अपने चरम तक जा पहुँची है। मानवीय प्रेम के उन्नत आदर्श की अवधारणा पूँजीवाद (वर्ग-समाज की अन्तिम मंजिल) के शैशव-काल में ही जन्म ले सकती थी। जीवन में हर चीज़ अपने प्रतिकूल पहलू के साथ ही अस्तित्व में आती है। पूँजीवादी समाज में व्यक्तित्व और मानवीय सारतत्व के चरम विघटन के साथ ही उनके निषेध के पहलू-उनके पुनस्संघटन के विचार और मार्ग को, अस्तित्व में आना था और फ़िर निश्चित ही इतिहास की गति उस दिशा में जायेगी जब यह दूसरा पहलू (सर्वहारा क्रान्ति के बाद और समाजवादी संक्रमण की दीर्घावधि के दौरान) प्रधान पहलू बन जायेगा, और वर्ग-विहीन समाज में निजी सम्पत्ति-सम्बन्धों के आधार और उससे उत्पन्न अधिरचना के पूर्ण विलोपन के बाद ही मनुष्य और सच्चे मानवीय प्यार के आदर्श सम्पूर्ण अर्थों में वस्तुगत यथार्थ बन सकेंगे।
एक और भ्रान्ति का निवारण यहाँ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पूँजीवादी सामाजिक श्रम-विभाजन के अन्तर्गत केवल मज़दूर ही मनुष्यता से, समाज से और मानवीय मूल्यों-भावनाओं से अलगाव का शिकार है। चूँकि श्रम-प्रक्रिया समाज का बुनियाद होती है, इसलिए मज़दूर का अलगाव सबसे बुनियादी अलगाव होता है। लेकिन समाज के अन्य वर्ग भी अलगाव और आत्म-अलगाव के समान रूप से शिकार होते हैं। शारीरिक श्रम करने वाले मज़दूर के अतिरिक्त मानसिक श्रम करने वाले और पूँजीवादी उत्पादन-तंत्र के प्रबन्धन–संचालन के दफ़्तरी कामों और पूरक सेवा-क्षेत्र से जुड़े मध्यवर्ग के लोग भी अपने कार्यकलापों के परिणाम से अपरिचित और विच्छिन्न होते हैं, वे उत्पादन-प्रक्रिया से विच्छिन्न होते हैं और सबसे नैसर्गिक मानवीय गुण-श्रम से विच्छिन्न होते हैं। इस नाते वे और अधिक मनोरोगी स्तर पर आत्म-अलगाव के शिकार होते हैं। जबतक मानसिक श्रम की श्रेष्ठता सहित सभी बुर्जुआ अधिकार और उनपर आधारित अन्तर्वैयक्तिक असमानताएँ बनी रहेंगी, तबतक यह स्थिति बनी रहेगी। पूँजीपति भी सामाजिक उत्पादन की बुनियादी कार्रवाई से पूर्णतः विच्छिन्न केवल अधिशेष निचोड़ने के लक्ष्य के लिए जीता है। पूँजी कोई चीज़ नहीं होती बल्कि वह समाज की सुनिश्चित ऐतिहासिक संरचना में निहित सुनिश्चित सामाजिक उत्पादन-सम्बन्ध होती है जो एक चीज़ के रूप में अभिव्यक्त होती है और उस चीज़ को विशिष्ट सामाजिक चरित्र देती है (विस्तृत विवेचना के लिए देखें, पूँजी, खण्ड-3, अध्याय-48)। पूँजीपति जिसका एकमात्र लक्ष्य पूँजी-संचय होता है, वह मनुष्य रह ही नहीं जाता। उसके लिए उत्पादन का लक्ष्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बल्कि मुनाफ़ा होता है। उसके सभी सपने और सुख की सभी अवधारणाएँ मुनाफ़ा के इर्द-गिर्द निर्मित होती है। वह स्वयं पूँजी का व्यक्ति-रूप ('कैपिटल परसॉनिफ़ायड') होता है। पत्नी भी उसके लिए अपने पूँजी-साम्राज्य का उत्तराधिकारी पैदा करने वाले उत्पादन के साधन से अधिक कुछ नहीं होती और उसे वह प्यार भी उसी रूप में करता है। पूँजी खुद जीन–लगाम कसकर पूँजीपति पर सवार उसे दिन-रात दौड़ाती रहती है। वह स्वयं अपनी आत्म अलगावग्रस्त चेतना से जिसे प्यार, आनन्द या जीवनोपभोग समझता है, वह वास्तव में एक विकृत और मिथ्या चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मार्क्स ने इस बात पर बल दिया कि बुर्जुआ समाज के सभी वर्गों के लोगों में व्याप्त अलगाव के सभी रूपों का आधार श्रम का अलगाव है। इसी के चलते वास्तविक, सामाजिक अन्तरविरोध विकृत और मिथ्या चेतना के रूप में परावर्तित, अभिव्यक्त और प्रतिफ़लित होते हैं।
अलगाव-विषयक इस पूरी चर्चा का उद्देश्य इस बात को स्पष्ट करना है कि बुर्जुआ समाज में सच्चे अर्थों में प्रेम की स्वतंत्रता सम्भव ही नहीं है। सामाजिक श्रम-विभाजन न केवल प्रेम, विवाह-सम्बन्ध और परिवार में स्त्री को बराबरी का दर्जा नहीं देता बल्कि मानवीय प्यार के आधुनिक मनुष्य के समक्ष उपस्थित आदर्श को जीवन का यथार्थ बनने की भी इज़ाज़त नहीं देता क्योंकि बुर्जुआ नागरिक (स्त्री-पुरुष) आत्म-अलगाव और भावना, सम्बन्ध आदि हर चीज़ को वस्तु के रूप में देखने की मानसिकता (रीइफ़िकेशन) से ग्रस्त होने के कारण प्यार करने में अक्षम है, वे आत्मनिर्वासित आत्माओं वाले लोग हैं। ज़ाहिर है कि बुर्जुआ श्रम-विभाजन की समाप्ति ही इस स्थिति को बदल सकती है। अतः किसी भी सूरत में, भारत जैसे देशों में आज भी मौजूद मध्ययुगीन बन्धनों के विरुद्ध विद्रोह की बात करते हुए बुर्जुआ प्रेम का आदर्शीकरण नहीं करना होगा, क्योंकि इसकी विद्रूपताएँ भी भारतीय जीवन का समकालीन यथार्थ बन चुकी हैं, (पश्चिम में तो पहले ही ऐसा हो चुका था)। हमें बुर्जुआ जनवाद के सीमान्तों का अतिक्रमण करना होगा और समाजवादी परियोजना के आत्मिक-सांस्कृतिक पक्षों पर सोचना होगा।
पूँजीवादी उत्पादन के क्षेत्र में श्रम-विभाजन जिस प्रकार समाज को शोषक-उत्पीड़क और शोषित-उत्पीड़ित के दो परस्पर–विरोधी पक्षों में बाँट देता है, उसी प्रकार यह परिवार के भीतर मानवीय पुनरुत्पादन के दायरे में भी स्त्री और पुरुष को क्रमशः गुलाम और मालिक का दर्जा दे देता है और इसी बुनियाद से ऐतिहासिक विकासक्रम में विकसित हुए प्रेम के दायरे में भी पुरुष को कृपाशील दाता और स्त्री को विवश और कृतज्ञ प्राप्तकर्ता बना देता है। स्त्री को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए किसी पुरुष को प्यार करने के मिथ्याभास में जीते हुए अन्ततः शरीर–समर्पण करना ही होता है। और पुरुष ऐसा अनुग्रह कई स्त्रियों पर करने के लिए स्वतंत्र होता है। वह ऐसा करने वाली स्त्री को "प्यार"करने की कृपा करता है और इस मायने में आदिम 'ईरोस'और व्यभिचार की मानसिकता में जीते हुए स्त्री को एक शरीर या सेक्स के मूर्त रूप से अधिक कुछ नहीं समझता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक बुर्जुआ नागरिक को सबसे अधिक ख़तरनाक स्त्री का स्वतंत्र व्यक्तित्व लगता है, पर विडम्बना यह है कि बुर्जुआ उत्पादन-प्रणाली की स्वतंत्र आन्तरिक गति से स्त्रियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व और स्वतंत्र अस्मिता का पैदा होना भी अपरिहार्य है। जो निकृष्टतम कोटि की उजरती गुलाम हैं उनमें यह स्वतंत्रता (आर्थिक स्वनिर्भरता के चलते) बुर्जुआ और मध्यवर्गीय स्त्रियों से (उनकी स्वतंत्र चेतना तो वस्तुतः एक विकृत या मिथ्याभासी चेतना है) कई गुना अधिक होती है और सर्वहारा पुरुष भी उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। जीवन–साथी चुनने-त्यागने या पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी के मामले में एक हद तक की वास्तविक आज़ादी यदि दीखती भी है तो सर्वहारा स्त्रियों में ही दीखती है। यानी बुर्जुआ समाज ने कथनी में प्यार करने के अधिकार को पुरुषों के साथ ही स्त्रियों का भी अधिकार माना, पर यह अधिकार एक सीमित हद तक यदि लागू भी हुआ तो उत्पीड़ित वर्ग के बीच ही, जबकि अन्य अधिकार शासक वर्ग तक सीमित बने रहे और उत्पीड़ित वर्ग से प्रत्यक्ष-परोक्ष ढंग से छीने जाते रहे। यह भी इतिहास का एक व्यंग्य ही है। कुछ निश्चित आर्थिक प्रभावों के कारण शोषक वर्गों में वास्तविक स्वेच्छा से जीवन–साथी के चुनाव या पारिवारिक निर्णयों में स्त्रियों की भागीदारी की मिसालें कम मिलती हैं, जबकि मेहनतकशों में स्थिति इसके विपरीत होती है (एंगेल्स: 'परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति', पूर्वोद्धृत, पृ- 96)। भारत में भी उभरता हुआ और संख्यात्मक रूप से बढ़ता हुआ सर्वहारा वर्ग जैसे-जैसे किसानी ज़मीन और संस्कारों से मुक्त होता जा रहा है और जैसे-जैसे स्त्रियों की भारी आबादी उजरती मज़दूरों की कतारों में शामिल होती जा रही हैं, वैसे-वैसे यह स्थिति ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होती जा रही है।
श्रम विभाजन से स्त्री की पारिवारिक गुलामी को जोड़ते हुए मार्क्स लिखते हैं: "श्रम-विभाजन, जिसमें ये सभी अन्तरविरोध अन्तर्निहित होते हैं और जो बदले में परिवार में श्रम के प्राकृतिक विभाजन पर तथा परस्पर विरोधी अलग-अलग परिवारों में समाज के पृथक्करण पर आधारित होता है, उसके साथ-साथ श्रम और उसके उत्पाद का और इसलिए सम्पत्ति का वितरण, और जाहिरा तौर पर परिमाणात्मक एवं गुणात्मक, दोनों ही रूपों में असमान वितरण, अस्तित्व में आता है: यही वह नाभिक है जिसका पहला रूप परिवार में मौजूद होता है, जहाँ पत्नी और बच्चे पति के गुलाम होते हैं। परिवार में यह प्रच्छन्न, हालाँकि फ़िर भी अत्यन्त भोंड़ी गुलामी ही पहली सम्पत्ति है…" (मार्क्स: 'जर्मन आइडियोलॉजी', पूर्वोद्धृत, पृ- 44)। आगे चलकर, निजी सम्पत्ति का अग्रवर्ती विकास ही पारिवारिक जीवन के रूपों के विकास को अनुकूलित करती है। परिवार राज्यसत्ता और नागरिक समाज का आधार होता है, पर निजी सम्पत्ति और श्रम-विभाजन इसे सामुदायिक चौहद्दी से बाहर (एक पृथक् घरेलू अर्थव्यवस्था के रूप में) एक निजी चीज़ बना देते हैं। परिवार ही वह व्यावहारिक बुनियाद है जिसपर बुर्जुआ वर्ग का आधिपत्य विकसित हुआ। (बुर्जुआ) परिवार की संस्था निहायत व्यावहारिक मामलों पर– आर्थिक मसलों पर टिकी होती है। बुर्जुआ समाज में परिवार की स्वतंत्र मान्यता या स्त्री-पुरुष की पारस्परिक चाहत नहीं बल्कि आम तौर पर बोरियत और वित्तीय हित ही लोगों को विवाह के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए, व्यवहारतः परिवार संस्था के सारहीन और विघटित हो जाने के बावजूद, औपचारिक रूप से यह बनी रहती है क्योंकि बुर्जुआ उत्पादन-प्रणाली और नागरिक समाज के लिए इसका बना रहना ज़रूरी है। उन्नीसवीं शताब्दी में ही फ्रांस और इंग्लैण्ड के समाजवादियों और जर्मन दार्शनिकों ने इस सच्चाई को रेखांकित किया था और आलोचनात्मक यथार्थवाद के पुरोधाओं ने अपने उपन्यासों में पारिवारिक जीवन के तनावों-त्रासदियों और विघटन की आन्तरिक गति को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया था। इसके चन्द उदाहरणों के तौर पर तोल्स्तोय की 'अन्ना कारेनिना', फ़ील्डिंग की 'टॉम जोन्स', जार्ज इलियट की 'मिडिल मार्च', गाल्सवर्दी की 'द फ़ोरसाइट सागा', हचिंसन की 'दिस फ्रीडम', स्टर्न की 'द मैट्रियार्क'और पर्लबक की 'ड्रैगन सीड'जैसी साहित्यिक कृतियों का नाम लिया जा सकता है। मार्क्स और एंगेल्स ने इसी आलोचना को एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक आधार पर आगे विकसित किया। परिवार के विघटन को उन्होंने दो रूपों में देखा: पहला, वह वास्तविक विघटन जो दरअसल हो रहा है क्योंकि स्वयं बुर्जुआ वर्ग इसका कर्त्ता है, और दूसरा वह आवश्यक या वांछनीय विघटन, जो इस स्थिति की सचेतन स्वीकृति और सर्वहारा क्रान्ति द्वारा शुरू की जाने वाली वि-अलगाव (डी–एलियनेशन) की प्रक्रिया द्वारा परिवार के बुर्जुआ स्वरूप के उन्मूलन की स्वीकृति पर आधारित है। सिद्धान्त और व्यवहार में परिवार यदि अभी भी मौजूद है तो इसलिए कि बुर्जुआ आधिपत्य इसी आधार पर टिका हुआ है। अपने अन्तर्य से ही पाखण्डी, बुर्जुआ मनुष्य इस संस्था की शर्तों का पालन नहीं करता, लेकिन फ़िर भी, आम तौर पर, इसे बनाये रखता है। व्यक्तियों के स्तर पर, सिद्धान्त और व्यवहार में, परिवार का निषेध किया जाता है, लेकिन समाज के स्तर पर, सिद्धान्त और व्यवहार में, इसे बरक़रार रखा जाता है। अलगावग्रस्त अस्तित्व की नीरसता और खालीपन, आर्थिक हित, विवाह और परिवार की तमाम सैद्धान्तिक आलोचनाओं और उनके व्यावहारिक टूटन के बावजूद पूँजीवादी उद्योग, व्यापार एवं वित्तीय तंत्र के मालिक और प्रबन्ध-तंत्र के कर्ता-धर्ता, बुर्जुआ राज्य मशीनरी के कर्ता-धर्ता बुर्जुआ नागरिक, बुर्जुआ स्वतंत्र पेशेवर लोग और बुर्जुआ बुद्धिजीवी विवाह एवं परिवार के वास्तविक विघटन की दिशा में कत्तई आगे नहीं बढ़ते। बुर्जुआ अस्तित्व का आम पाखण्ड दो सेक्सों के बीच सम्बन्ध का एक काल्पनिक पवित्र संसार रचता है, जो विमानवीकृत 'रीइफ़िकेशन'के रूप में कायम अपनी वास्तविकता में वस्तुतः एक कुरूप और गन्दी चीज़ होती है। और वही पाखण्ड, जीवन की कुरूप आनुभविक सच्चाई पर निर्भर होने के नाते, विवाह और परिवार की वचनबद्धता से पलायन और आपातकालीन निकास-द्वार के रूप में बदचलनी, नाजायज़ रिश्तों और वेश्यागमन का इस्तेमाल करता है। बुर्जुआ समाज में रहते हुए शासकवर्ग के वर्चस्वशील मूल्यों और संस्कृति के शिकार मेहनतकश भी होते हैं, जीवन का खालीपन उन्हें भी विमानवीकृत और अलगावग्रस्त करके व्यभिचार-अनाचार की ओर धकेलता है, लेकिन निजी सम्पत्ति से जुड़ा कोई आर्थिक हित नहीं होने के कारण रिश्ते बनाने, चलाने और तोड़ने के मामले में उनके जीवन में स्वेच्छा का तत्व अधिक काम करता है। दूसरे, उनके वहाँ व्याप्त व्यभिचार और जीवन की कुरूपता पर पाखण्ड का कोई पर्दा नहीं होता। इस मायने में सापेक्षतः उनका जीवन नैतिक अधिक होता है। हाँ, भारत जैसे पिछड़े पूँजीवादी समाजों में, मेहनतकश जीवन में जाति-धर्म आदि की प्राक्पूँजीवादी जकड़बन्दी की घुटनभरी सड़ांध ज़रूर अभी भी मौजूद है, जिस बुराई को पूँजीवाद अपना भी रहा है तथा बुर्जुआ बुराई द्वारा विस्थापित भी कर रहा है।
बुर्जुआ नागरिक जब स्त्री को भोग्या, दासी और आनन्दोपभोग की वस्तु मानता है, तो मार्क्स के अनुसार वह अपने स्वयं के ही सीमाहीन पतन, अलगाव और अलगावजन्य विमानवीकरण को अभिव्यक्त करता है। विवाहेतर यौन-सम्बन्ध, विशेषकर हर नये-पुराने रूप के वेश्यागमन में मनुष्य की सच्ची सामाजिक प्रकृति का यह अलगाव सर्वाधिक सघन एवं प्रातिनिधिक अभिव्यक्ति पाता है क्योंकि वेश्यावृत्ति एक ऐसे व्यापारिक रिश्ते पर आधारित होती है जो वेश्या स्त्री से अधिक, उसके पास जाने वाले पुरुष को अलगावग्रस्त और आत्म-अलगाव का शिकार बनाती है, उसे एक ऐसी अन्तरात्मा बना देती है जो मालों के द्वीप पर आत्मनिर्वासित है जहाँ खरीद-फ़रोख़्त के अतिरिक्त और कोई मानवीय भावनात्मक क्रिया-व्यापार होता ही नहीं। अपने इर्द-गिर्द के सभ्य समाज में चल रही पार्टियों, इण्टरनेट और ब्लू फ़िल्मों द्वारा परोसी जा रही यौन विकृतियों, बुर्जुआ कारोबारों के ऑफ़िसों, क्लबों-रिसार्टों, मसाज सेण्टरों और कालगर्ल्स की दुनिया पर निगाह डालिये, आपको इस बात की सच्चाई का सहज अहसास हो जायेगा। बुर्जुआ समाज का यह सूत्र-वाक्य है कि सब कुछ खरीद पाने की शक्ति रखने वाली मुद्रा मानवीय भावनाओं, रिश्तों और प्यार को भी खरीद सकती है। जैसा कि मार्क्स बताते हैं, मुद्रा स्वयं एक सार्वभौमिक वेश्या है और कौमों और राष्ट्रों की सर्वसामान्य कुटनी है जो मानवीय आवश्यकता और उसकी पूर्ति के साधनों के बीच, मनुष्य और उसके जीवन के बीच, एक मनुष्य और अन्य मनुष्यों के बीच सौदेबाज़ी कराने और रिश्ते पटाने का काम करती है। मुद्रा प्राणियों और सामुदायिक मानव जाति के सभी नैसर्गिक गुणों को गड्डमड्ड कर देती है, उन्हें उलट देती है और उनके वैपरीत्यों के साथ उनका विनिमय कर देती है। "यह अन्तरविरोधों को आपस में आलिंगनबद्ध करा देती है।"आगे मार्क्स लिखते हैं: "मनुष्य को मनुष्य और संसार के साथ उसके सम्बन्धों को आप मानवीय मान लीजिए: तब फ़िर आप प्रेम का केवल प्रेम के साथ, विश्वास का विश्वास के साथ, आदि-आदि… विनिमय कर सकते हैं। यदि आप कला का आस्वादन करना चाहते हैं तो आपको कलात्मक दृष्टि से परिष्कृत व्यक्ति होना चाहिए, यदि आप दूसरे लोगों पर प्रभाव डालना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों पर स्फ़ूर्तिप्रद और उत्साहवद्धर्क प्रभाव डालने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मनुष्य और प्रकृति के साथ, आपके प्रत्येक सम्बन्ध को, आपकी कामना की वस्तु के अनुरूप, आपके वास्तविक वैयक्तिक जीवन की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यदि आप बदले में प्रेम जगाये बिना प्रेम करते हैं-यानी अगर प्रेम के रूप में आपका प्रेम जवाबी प्रेम नहीं पैदा करता; यदि प्रेम करने वाले एक व्यक्ति के रूप में आप स्वयं की एक जीवन्त अभिव्यक्ति के रूप में अपने को प्रेम पाने वाला व्यक्ति नहीं बना पाते, तो आपका प्यार निश्शक्त है-एक दुर्भाग्य है" (मार्क्स: दि इकोनॉमिक एण्ड फ़िलॉसोफ़िक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844, पूर्वोद्धृत, पृ- 169)।
स्त्री-पुरुष के बीच अन्योन्य क्रिया के रूप में प्यार और पूरी बराबरी और आज़ादी पर आधारित भावनात्मक-दैहिक सम्बन्ध को सम्भव बनाने के लिए उनके सम्बन्ध को अलगाव-मुक्त (डीएलियनेट) करना अपरिहार्य है तथा विवाह के सभी बुर्जुआ रूपों को-उनकी पूर्वशर्तों, परिस्थितियों और परिणतियों समेत-अन्तर्वस्तु एवं रूप की दृष्टि से बदलना अपरिहार्य है। चूँकि परिवार भी एक विशिष्ट उत्पादन-प्रणाली है और इसके आम नियमों से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए निजी सम्पत्ति और पृथक्कृत आर्थिक जीवन के उन्मूलन को परिवार के उन्मूलन से अलग करके नहीं देखा जा सकता (मार्क्स-एंगेल्स: 'जर्मन आइडियोलॉजी', पूवोद्धृत, पृ- 40, पृष्ठ के नीचे दी गयी टिप्पणी से)। मार्क्स के अनुसार निजी सम्पत्ति का सकारात्मक, प्रभावी उन्मूलन ही समग्रता में सच्चे मानव जीवन की प्राप्ति और सभी अलगावों का आमूलगामी उन्मूलन है। इस प्रकार, स्त्री-पुरुष अपने जीवन और सम्बन्धों में अपने मानवीय अस्तित्व को साकार कर सकेंगे और उनका जीवन और बुर्जुआ परिवार का स्थान लेने वाली पारिवारिक इकाई अनिवार्यतः वैयक्तिक और सामुदायिक-एक ही साथ दोनों होगी। विवाह के उन्मूलन का अर्थ किसी भी रूप में स्त्री का सामुदायिक दर्जा नहीं होगा, मानो कि वह कोई साझा सम्पत्ति हो, जैसा कि "भोंड़े और विचारहीन कम्युनिज़्म"की प्रत्येक धारा का मानना था (मार्क्स: 'दि इकोनॉमिक एण्ड फ़िलॉसोफ़िक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844, पृ- 133)। सवाल यहाँ निजी सम्पत्ति के उन्मूलन का है, न कि उसके सामान्यीकरण और विस्तार का है। मार्क्स यहाँ पूँजीवाद के सार्वत्रीकरण के लिए पूर्ववर्ती भोंड़े कम्युनिज़्म की आलोचना करते हैं क्योंकि यह मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रतिकूल है और समतलीकरण की किसी प्रक्रिया द्वारा मनुष्य की स्थिति का निर्धारण मनुष्य की विशिष्ट प्रकृति से कदापि मेल नहीं खाता। स्त्री-पुरुष सम्बन्धों में मानवीय अलगाव से मुक्ति मनुष्य के "मानवीय, यानी सामाजिक अस्तित्व"को बहाल करना है (मार्क्स: वही)।
सामाजिक संरचनागत उपादानों को अलग करके देखें, तो मार्क्स का यह कहना सही है कि "सेक्सुअल क्रियाकलाप शरीर का सर्वोच्च कार्य है" (मार्क्स: 'हेगेल्स फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ राइट', पृ- 40, कैम्ब्रिज, 1970)। लेकिन सेक्सुअल क्रियाकलाप को मार्क्स एक पाश्विक क्रिया या सम्भोग की क्रिया के रूप में नहीं देखते। वास्तविक व्यक्तिगत यौन–प्रेम में मार्क्स दैहिक आकर्षण और तज्जन्य सौन्दर्यात्मक-आत्मिक मनोभावों का संश्लिष्ट अमूर्तन देखते हैं, जहाँ रुचियों और विचारों की एकता के बिना, मात्र साहचर्य से यौनाकर्षण नहीं उत्पन्न होता। मार्क्स मानवीय सेक्सुअल क्रियाकलाप को विरुपित करने वाली और उसका दम घोंट देने वाली निजी सम्पत्ति की सत्ता और तज्जन्य अलगाव को अनावृत्त करते हैं। निजी सम्पत्ति के सामान्यीकरण के नियम के लिए हर विशिष्ट मानवीय परिघटना को एक नज़ीर बनाना पूँजीवाद का ही सार्वत्रीकरण हैं, और इसके बजाय मार्क्स एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जहाँ हर ठोस मानवीय परिघटना या सम्बन्ध सार्वत्रिक मानवीय प्राकृतिक परिवेश को प्रतिबिम्बित करता हो। वे लिखते हैं: "स्त्री को सामुदायिक काम-वासना की तृप्ति का माल और दासी समझने के दृष्टिकोण में वह असीमित अधःपतन अभिव्यक्त होता है जिसमें पुरुष सिर्फ़ अपने लिए अस्तित्वमान है, क्योंकि इस दृष्टिकोण के रहस्य की असंदिग्ध, निर्णायक, सुस्पष्ट और अप्रच्छन्न अभिव्यक्ति पुरुष के स्त्री के साथ सम्बन्ध में और उस ढंग में सामने आती है जिसमें प्रत्यक्ष तथा प्राकृतिक जातिमूल-सम्बन्धी रिश्ते (स्पेसीज़ रिलेशनशिप) की कल्पना की जाती है। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष, प्राकृतिक और आवश्यक सम्बन्ध पुरुष का स्त्री से सम्बन्ध है। इस नैसर्गिक जाति-मूल सम्बन्धी रिश्ते के अन्तर्गत मनुष्य का प्रकृति के साथ सम्बन्ध सीधे उनका मनुष्य के साथ सम्बन्ध है, ठीक वैसे ही जैसे उसका मनुष्य के साथ सम्बन्ध सीधे प्रकृति के साथ उसका सम्बन्ध है-जो उसका नैसर्गिक लक्ष्य (नेचुरल डेस्टिनेशन) है। अतः इस रिश्ते में, जिस हद तक मानवीय सारतत्व मनुष्य के लिए प्रकृति बन गया है, उस हद तक ऐन्द्रिक रूप में (सेक्सुअली) अभिव्यक्त, प्रेक्षणीय तथ्य में परिणत होता है। इसलिए इस रिश्ते से मनुष्य के विकास के समग्र स्तर को जाना जा सकता है। इस रिश्ते के चरित्र से यह पता चलता है कि एक जाति-मूल प्राणी (स्पेसीज़-बीइंग) के रूप में, मनुष्य के रूप में मनुष्य स्वयं किस हद तक बन गया है और किस हद तक स्वयं को समझने लगा है, पुरुष का स्त्री के साथ सम्बन्ध मानव-प्राणी का मानव प्राणी के साथ सबसे प्राकृतिक सम्बन्ध है अतः यह इस बात को बतलाता है कि मनुष्य का स्वाभाविक आचरण किस हद तक मानवीय बन गया है, अथवा उसके भीतर का मानवीय सारतत्व किस हद तक प्राकृतिक सारतत्व बन गया है-किस हद तक उसकी मानवीय प्रकृति उसके लिए प्राकृतिक बन गयी है। यह रिश्ता यह भी प्रकट करता है कि किस हद तक मनुष्य की आवश्यकता एक मानवीय आवश्यकता बन गयी है, अतः किस हद तक व्यक्ति के नाते दूसरा व्यक्ति उसके लिए एक आवश्यकता बन गया है-किस हद तक अपने वैयक्तिक अस्तित्व के साथ-साथ वह एक सामाजिक प्राणी बन गया है" (मार्क्स: मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ़ 1844, पूवोद्धृत, पृ- 134)।
मार्क्स की यह तार्किक धारणा पूँजीवादी समाज की आन्तरिक गतिकी के अध्ययन का ही परिणाम थी कि बुर्जुआ उत्पादन-प्रणाली और अलगाव की अनिवार्य समाप्ति के बाद, विवाह और परिवार के बुर्जुआ स्वरूप का भी उन्मूलन हो जायेगा, स्त्री-पुरुष स्वतंत्रता और समानता के साथ जोड़े बनायेंगे, स्त्रियाँ तब भोग एवं उत्पादन-पुनरुत्पादन का साधन नहीं होंगी, वे पुरुषों पर निर्भर नहीं होंगी, दम्पति नागरिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होंगे, बच्चे अपने माता-पिता पर निर्भर नहीं होंगे और चूल्हे-चौकठ की दासता से मुक्त स्त्रियाँ सभी उत्पादक एवं सामाजिक कार्रवाइयों में बराबर की भागीदार होंगी। जैसा कि हम एंगेल्स को पहले ही उद्धृत कर चुके हैं, ये जीवन स्थितियाँ स्वच्छन्द यौन-सम्बन्धों को नहीं बल्कि एकान्तिक, एकनिष्ठ यौन–प्रेम और दाम्पत्य को जन्म देंगी क्योंकि यौन–प्रेम अपनी प्रकृति से ही एकान्तिक होता है। न केवल भोंड़े कम्युनिज़्म के प्रवर्तकों ने और अराजकतावादियों ने यौन सम्बन्धों की स्वच्छन्दता की बात की, बल्कि बुर्जुआ वर्ग मार्क्स के ज़माने से लेकर आजतक कम्युनिस्टों द्वारा "यौन–मुक्ति"और स्त्रियों के समाजीकरण का शोर मचाता रहा है (तथा बुर्जुआ नारीवादी भी स्त्री-दासता का कारण ऐतिहासिक-सामाजिक स्थितियों में नहीं बल्कि यौन भेद में देखते हुए "यौन–मुक्ति"के विविधरूपा विचार आज भी प्रस्तुत करती रहती हैं)। मार्क्स ने 1848 में इन कूपमण्डूकता और कुत्सापूर्ण अटकलों-तोहमतों का जो उत्तर दिया था, उसे इस पर और अधिक स्पष्टता के लिए हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं:
"बुर्जुआ अपनी पत्नी को एक उत्पादनोपकरण के सिवा और कुछ नहीं समझता। उसने सुन रखा है कि उत्पादन उपकरणों का सामूहिक रूप से उपयोग होगा और, स्वभावतः, वह इसके अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाता कि सभी चीज़ों की तरह औरतें भी सभी के साझे की हो जायेंगी।
"वह यह सोच भी नहीं सकता कि दरअसल मक़सद यह है कि आम उत्पादन उपकरण होने की स्थिति का ही ख़ात्मा कर दिया जाये।
"बाकी तो बात यह है कि हमारे बुर्जुआ के औरतों के समाजीकरण के ख़िलाफ़, जो उसके दावे के मुताबिक कम्युनिस्टों द्वारा खुल्लमखुल्ला और आधिकारिक रूप से स्थापित किया जायेगा, सदाचारी आक्रोश से अधिक हास्यास्पद दूसरी और कोई चीज़ नहीं है। कम्युनिस्टों को स्त्रियों का समाजीकरण प्रचलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है; उनकी यह स्थिति तो लगभग अनादि काल से चली आ रही है।
"हमारे बुर्जुआ इसी से सन्तोष न करके कि वे अपने मज़दूरों की बहू-बेटियों का अपनी मरज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, सामान्य वेश्याओं की तो बात ही क्या, एक-दूसरे की बीवियों पर हाथ साफ़ करने में विशेष आनन्द प्राप्त करते हैं।
"बुर्जुआ विवाह वास्तव में साझे की पत्नियों की ही व्यवस्था है, इसलिए कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ अधिक से अधिक यही आरोप लगाया जा सकता है कि वे स्त्रियों के पाखण्ड पूर्वक छिपाये गये समाजीकरण की जगह खुले तौर पर क़ानूनी समाजीकरण लाना चाहते हैं। बाकी तो यह बात अपने आप में साफ़ है कि वर्तमान उत्पादन-पद्धति के उन्मूलन के साथ-साथ इस पद्धति से उत्पन्न स्त्रियों के समाजीकरण का, अर्थात खुली और ख़ानगी, दोनों ही प्रकार की वेश्यावृत्ति का अनिवार्यतः उन्मूलन हो जायेगा।" (मार्क्स-एंगेल्स 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र', पृ- 52, राहुल फ़ाउण्डेशन, लखनऊ, 1999)
एक वर्ग-विहीन समाज में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध से कौन-सी विकृतियाँ समाप्त हो जायेंगी, इसके बारे में आज की ज़मीन पर खड़ा होकर तो बस इतना ही तर्कसंगत अनुमान लगाया जा सकता है। प्रश्न की और अधिक स्पष्ट समझ के लिए कम्युनिस्ट भविष्य के बारे में हम एक बार फ़िर एंगेल्स को उद्धृत करना चाहेंगे:
"…एकनिष्ठ विवाह से वे सारी विशेषताएँ निश्चित रूप से मिट जायेंगी जो स्वामित्व-सम्बन्धों से उसके उत्पन्न होने के कारण पैदा हो गयी हैं। ये विशेषताएँ हैं: एक तो पुरुष का आधिपत्य, और दूसरे विवाह सम्बन्ध का अविच्छेद्य रूप। दाम्पत्य जीवन में पुरुष का अधिपत्य केवल उसके आर्थिक प्रभुत्व का एक परिणाम है और उस प्रभुत्व के मिटने पर वह अपने आप खतम हो जायेगा। विवाह-सम्बन्ध का अविच्छेद्य रूप कुछ हद तक उन आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है जिनमें एकनिष्ठ विवाह की उत्पत्ति हुई थी और कुछ हद तक वह उस समय से चली आती हुई एक परम्परा है जबकि इन आर्थिक परिस्थितियों तथा एकनिष्ठ विवाह के सम्बन्ध को ठीक-ठीक नहीं समझा जाता था और धर्म ने उसे अतिरंजित कर दिया था। आज इस परम्परा में हज़ारों दरारें पड़ चुकी हैं। यदि प्रेम पर आधारित विवाह ही नैतिक होते हैं तो ज़ाहिर है कि केवल वे विवाह ही नैतिक माने जायेंगे जिनमें प्रेम कायम रहता है। व्यक्तिगत यौन–प्रेम के आवेग की अवधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। विशेषकर पुरुषों में तो इस मामले में बहुत ही अन्तर होता है। और प्रेम के निश्चित रूप से नष्ट हो जाने पर या किसी और व्यक्ति से उत्कट प्रेम हो जाने पर पति-पत्नी का अलग हो जाना दोनों पक्ष के लिए और समाज के लिए भी हितकारक बन जाता है। अलबत्ता, लोग तलाक की कार्रवाइयों के व्यर्थ के झंझटों से बच जायेंगे।
"अतएव, पूँजीवादी उत्पादन के आसन्न विनाश के बाद यौन-सम्बन्धों का स्वरूप क्या होगा, उसके बारे में आज हम केवल नकारात्मक अनुमान कर सकते हैं-अभी हम केवल इतना कह सकते हैं कि क्या चीज़ें तब नहीं रहेंगी। परन्तु उसमें कौन सी नयी चीज़ें जुड़ जायेंगी? यह उस समय निश्चित होगा जब एक नयी पीढ़ी पनपेगी-ऐसे पुरुषों की पीढ़ी जिसे जीवन भर कभी किसी नारी की देह को पैसा देकर या सामाजिक शक्ति के किसी अन्य साधन के द्वारा खरीदने का मौक़ा नहीं मिलेगा, और ऐसी नारियों की पीढ़ी जिसे कभी सच्चे प्रेम के सिवा और किसी कारण से किसी पुरुष के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा, और न ही जिसे आर्थिक परिणामों के भय से अपने को अपने प्रेमी के सामने आत्मसमर्पण करने से कभी रोकना पड़ेगा। और जब एक बार ऐसे स्त्री-पुरुष इस दुनिया में जन्म ले लेंगे, तब वे इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं करेंगे कि आज हमारी राय में उन्हें क्या करना चाहिए। वे स्वयं तय करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और उसके अनुसार वे स्वयं ही प्रत्येक व्यक्ति के आचरण के बारे में जनमत का निर्माण करेंगे-और बस, मामला खतम हो जायेगा।" (फ्रे- एंगेल्स: 'परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति', मार्क्स-एंगेल्स: संकलित रचनाएँ, खण्ड-3, भाग-2, पूर्वोद्धृत, पृ- 97–98)
http://ahwanmag.com/archives/4889
आह्वान'के पाठकों से एक अपील
दोस्तों,
"आह्वान"सारे देश में चल रहे वैकल्पिक मीडिया के प्रयासों की एक कड़ी है। हम सत्ता प्रतिष्ठानों, फ़ण्डिंग एजेंसियों, पूँजीवादी घरानों एवं चुनावी राजनीतिक दलों से किसी भी रूप में आर्थिक सहयोग लेना घोर अनर्थकारी मानते हैं। हमारी दृढ़ मान्यता है कि जनता का वैकल्पिक मीडिया सिर्फ जन संसाधनों के बूते खड़ा किया जाना चाहिए।
एक लम्बे समय से बिना किसी किस्म का समझौता किये "आह्वान"सतत प्रचारित-प्रकाशित हो रही है। आपको मालूम हो कि विगत कई अंकों से पत्रिका आर्थिक संकट का सामना कर रही है। ऐसे में "आह्वान"अपने तमाम पाठकों, सहयोगियों से सहयोग की अपेक्षा करती है। हम आप सभी सहयोगियों, शुभचिन्तकों से अपील करते हैं कि वे अपनी ओर से अधिकतम सम्भव आर्थिक सहयोग भेजकर परिवर्तन के इस हथियार को मज़बूती प्रदान करें।
आप -
1- आजीवन सदस्यता ग्रहण कर सहयोग कर सकते हैं।
2- अपने मित्रों को "आह्वान"की सदस्यता दिलवायें।
3- "आह्वान"के मद में आर्थिक सहयोग भेजें। और "आह्वान"के वितरण में लगे सहयोगियों से अपील है कि वे पत्रिका की भुगतान राशि यथासम्भव शीघ्र प्रेषित कराने की व्यवस्था करें।
ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें


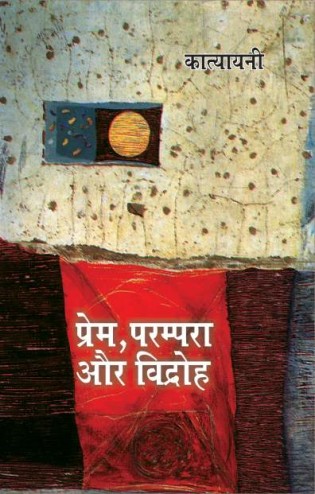

.jpg)












